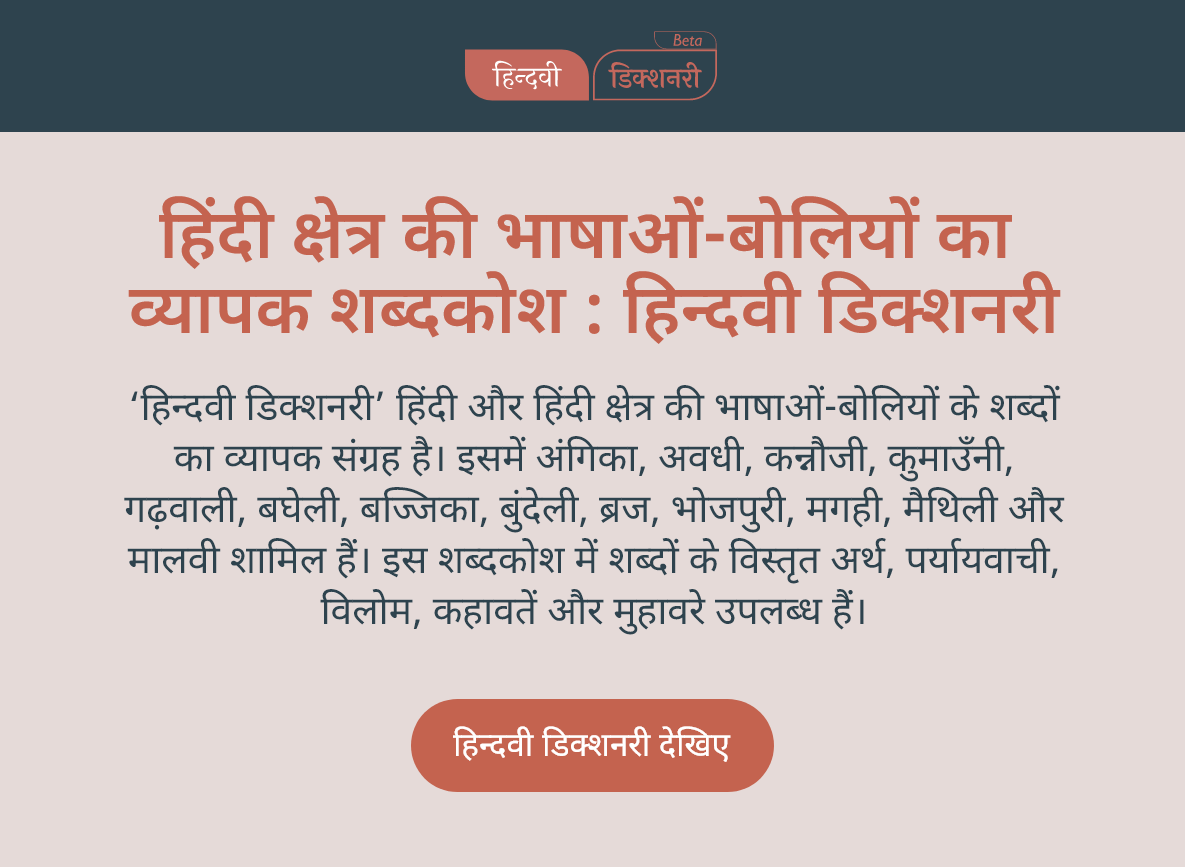रसखान
raskhan
सैयद इब्राहिम रसखान (1533-1628 ई.) हिंदी के उन मुसलमान कृष्णभक्त कवियों में सर्वोपरि हैं, जिन्होंने इस्लाम के बजाए धर्म का हिंदू रूप अंगीकृत किया। यह रहस्य है कि मुसलमान होते हुए भी वे कृष्णभक्ति की ओर कैसे आकृष्ट हुए? यह भी आश्चर्य है कि उनकी कविता में उनके मुसलमान होने का कोई संस्कार और चेतना नहीं है। वे आकंठ कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। शिवसिंह सेंगर ने उनके संबंध में लिखा है कि “ये मुसलमान कवि थे। श्री वृंदावन में जाकर ऐसे डूबे कि मुसलमानी धर्म त्यागकर मालाकंठी धारण किए हुए वृंदावन की रज में मिल गए। इनकी कविता निपट ललितमाधुरी से भरी हुई है।” भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी कविता पर मुग्ध और अभिभूत थे। उन्होंने अन्य मुसलमान कवियों के साथ रसखान को स्मरण करते हुए लिखा कि “इन मुसलमान हरिजनन पै कौटिन हिंदू वारिये।” अर्थात् इन मुसलमान ईश्वर भक्तों पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। रसखान उस समय हुए जब भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और उसके मानने वाले यहाँ के शासक थे। रसखान का होना इस बात का सबूत है कि यह ऐसा समय था, जब दो धर्मों के बीच दीवारें और दूरियाँ नहीं बनी थीं। रसखान को देशज भक्ति साहित्यिक रचनाओं में बहुत सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया है। रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य और असाधारण है—लगता है, वे कृष्ण, राधा और गोपियों के चित्त में डूबकर उनके जैसे हो गए हैं। उनकी रचनाओं में इसीलिए इन सबकी चित्तवृत्तियों का सूक्ष्म और हृदयस्पर्शी वर्णन मिलता है। रसखान कृष्णभक्त ही नहीं थे, वे ब्रजभाषा की सरस कवित-सवैया परंपरा से अवगत और इसमें निष्णात थे। उनकी भाषा का अर्थ गांभीर्य और माधुर्य किसी भी कृष्णभक्त कवि से कम नहीं है।
एक
रसखान के संबंध में बहुत कम ज्ञात है और उनसे संबंधित स्रोत भी सीमित हैं। कुछ अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनके जीवन की रूपरेखा का केवल अनुमान किया जा सकता है। उनका उल्लेख हरिदासी संप्रदाय से संबंधित भगवत रसिक (1692-1758 ई.) की रचना अनन्यनिश्चयात्म की आरंभिक भक्तनामावली (1537-1643 ई.), गोकुलनाथ (1551-1610 ई.) कथित और हरिराय (1551-1610 ई.) द्वारा संकलित दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, वेणीमाधवदास रचित मूल गुसाईंचरित (1687 ई.), राधाचरण गोस्वामी (1859-1925 ई.) की नवभक्तमाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-1885 ई.) की उत्तरार्धभक्तमाल (1976-77 ई.) में मिलता है। कदाचित् भक्त के रूप में रसखान उल्लेख और कई भक्तों के साथ भगवत रसिक ने पहली बार किया। उन्होंने भक्तनामावली के आरंभ में लिखा है कि “हमसौं इन साधुन सौं पंगति।” अर्थात् हमारा इन साधुओं के साथ व्यवहार और चाल-चलन है। इसके बाद उन्होंने बहुत उदारतापूर्वक अकबर, तानसेन, करमेती, मीरांबाई, रत्नावती और मीर माधव के साथ रसखान का भी नाम लिया है। शिवसिंह सेंगर ने लिखा है कि इनकी कथा भक्तमाल में पढ़ने योग्य है, लेकिन नाभादास की भक्तमाल (1594 ई.) और इसकी टीका भक्तिरसबोधिनी (1712 ई.) के ‘श्रीब्रजचंद्र के षोडस सखा’ (170) में केवल रसदान का उल्लेख मिलता है। यह अलग बात है कि भक्तमाल के संपादक भगवान्प्रसाद रूपकला ने अनुक्रमणिका में ‘रसखानरसदानजी’ लिखा है। वेणीमाधवदास के मूल गुसाईंचरित्र में भी रसखान का उल्लेख आया है। वेणीमाधवदास के अनुसार रचना के बाद तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे पहले सुनने वालों में रसखान भी सम्मिलित थे। उन्होंने लिखा है—
स्वामि नंद सुलाल को शिष्य पुनी तिसु नाम दयाल सुदास गुनि।
लिखिकै सोइ पोथो स्वठाम गए। गुरु के ढिग जाए सुनाम दियो।
यमुना तट पै त्रय वत्सर लौं। रसखानहिं जाए सुनावत भौ।
आशय यह है रामचरितमानस की समाप्ति के बाद सबसे पहले इसका श्रवण मिथिला के रूपारण स्वामी ने किया, उनके बाद संडीले के नंदलाल स्वामी ने सुना और उनके बाद नंदलाल के शिष्य सुदास द्वारा रसखान इसे यमुना नदी के तट पर तीन वर्ष तक सुनते रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस वेणीमाधवदास के अनुसार वि.सं. 1633 (1576 ई.) में पूर्ण की। रसखान 1557 ई. के आसपास यदि वृंदावन चले गए, तो संभव है कि उन्होंने यमुना तट पर रामचरितमानस सुनी होगी। यह अलग बात है कि कुछ विद्वान् वेणीमाधवदास की रचना मूल गुसाईंचरित को अप्रामाणिक मानते हैं। दो सौ बावन वैष्णवन वार्ता के बाद राधाचरण गोस्वामी का नवभक्तमाल में रसखान के संबंध में किया गया उल्लेख सबसे विस्तृत है। उन्होंने लिखा है—
दिल्ली नगर निवास बादसा बसं-बिभाकर।
चित्र देखि मन हरो, भरो मन प्रेम सुधाकर॥
श्री गोवर्धन आए जबै दरसन नहिं पाये।
टेढे मेढे बचन रचन निरभय ह्वै गाए॥
तब आप आप सुमनाय करि सुश्रुषा महमान की।
कवि कौन मिताई कहि सकै श्रीनाथ साथ रसखान की॥
अर्थात् रसखान दिल्ली नगर में निवासी थे। बादशाह वंश के सूर्य थे। कृष्ण का चित्र देखकर उस पर आसक्त हुए और प्रेम के चंद्रमा कृष्ण के प्रेम से मन भर गया। श्रीगोवर्धन आए और उनको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो टेढ़े-मेढ़ वचनों में निर्भय होकर रचना करने लगे। तब लोगों ने उनको समझकर उनका आतिथ्य किया। ऐसा कवि कौन है, जो उनकी श्रीनाथजी के साथ मित्रता का वर्णन कर सके। रसखान के संबंध में कई जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं।
दो
प्रेमवाटिका की रचना और वृंदावन आगमन के उल्लेख और विट्ठलनाथ की ज्ञात मृत्युतिथि के आधार पर रसखान के जीवन की रूपरेखा निर्धारित की गई है, लेकिन विद्वानों में इन उल्लेखों के निहितार्थ को लेकर पर्याप्त मतभेद है। प्रेमवाटिका में इसके रचना समय के संबंध में एक उल्लेख है। रसखान ने लिखा है कि “बिधु सागर रस इंदु सुभ, बरस सरस रसखानि। / प्रेमबाटिका रचि रुचिर, चिर हिय हरख बखान॥” यह रचना समय के उल्लेख की पारंपरिक पद्धति है और इसमें अंकों का उल्लेख प्रतीकात्मक होता है और उन्हें उल्टा पढ़ा जाता है। यहाँ विधु का प्रतीकार्थ एक, सागर का सात, रस का छह और इंदु का एक है। उल्टा पढ़ने पर इसका आशय वि.सं. 1671 (1614 ई.) है। विद्वानों में मतभेद यह है कि संस्कृत में सागर का उल्लेख चार के रूप में होता है। बाणभट्ट की कादंबरी में सागर चार ही माने गए हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान् प्रेमवाटिका की रचना का समय वि.सं. 1641 (1584 ई.) मानते हैं। कुछ अन्य का मानना है कि हिंदी की परंपरा में सागर का प्रतीकार्थ सात होता है। रसखान के समकालीन तुलसीदास (1511-1623 ई.) ने भी सागर सात माने हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि “भूमि सप्त सागर में चला। एक भूप रघुपति कोसला॥” (रामचरितमानस, 11/1 'उत्तरकांड') यदि हिंदी की परंपरा को प्रमाण माना जाए, तो प्रेमवाटिका का रचना समय वि.सं. 1671 (1614 ई.) होगा। विद्वानों की राय यह है कि इस संबंध में संस्कृत के बजाए हिंदी की परंपरा का ही विश्वास किया जाना चाहिए।
रसखान के वृंदावन आगमन के संबंध में प्रेमवाटिका में अंतःसाक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसके भी निहितार्थ को लेकर विद्वान् एकमत नहीं हैं। रसखान ने प्रेमवाटिका के एक दोहे में लिखा है कि “देखि गदर हित साहबी, दिल्लीह नगर मसान। / छिनहिं बादसा-बंस की, ठसक छोरि रसखान॥” इन पंक्तियों में जिस बादशाही के लिए ग़दर का उल्लेख है, वह कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों की राय अलग-अलग है। विश्वनाथप्रसाद मिश्र के अनुसार यह ग़दर अकबर (1542-1605 ई.) के शासनकाल में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग़दर 1554 और 1557 ई. के बीच हुआ। दरअसल अकबर के सत्तारूढ़ होने के बाद ग़दर और उसके कारण दिल्ली के श्मशान हो जाने जैसी स्थिति नहीं आई। देवेंद्रप्रसाद उपाध्याय की राय ही इस संबंध में युक्तिसंगत लगती है। अकबर से पहले पठानों के बीच सत्ता के लिए हुए संघर्ष और 1555 ई. में पड़े भयंकर अकाल से दिल्ली की स्थिति श्मशान जैसी हो गई थी। शेरशाह सूरि के उत्तराधिकार के लिए पठानों के बीच 1554 से 1557 ई. के बीच ज़बरदस्त सत्ता संघर्ष हुआ। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लामशाह (जलाल ख़ान, 1545-1554 ई.) की 1554 ई. में मृत्यु के बाद उसका बेटा फ़िरोज़शाह सत्तारूढ़ हुआ। एक माह बाद ही इस्लामशाह के साले मुबारिक ख़ाँ ने उसकी हत्या कर दी और वह आदिलशाह के नाम से सत्तारूढ़ हो गया। उसने दिल्ली पहुँचकर बादशाह की सेना को परास्त कर दिया। आदिलशाह का चचेरा भाई और बहनोई अहमद उसको परास्त कर सिकंदरशाह के नाम से सत्तारूढ़ हुआ। सिकंदरशाह के सत्तारूढ़ होने के बाद हुमायूँ ने 1555 ई. में दीयलपुर में अफ़गानों को हराया और उसने सरहिंद पहुँचकर सिकंदरशाह को पराजित कर दिया। केवल चार-पाँच महीने के दौरान दिल्ली की बादशाहत के लिए, जो हुआ वह दिल्ली को उजाड़ देने के लिए पर्याप्त था। देवेंद्रप्रताप उपाध्याय ने लिखा है कि “चार-पाँच महीने में तीन-तीन हुकूमतें बदलीं, इसे ग़दर नहीं तो क्या कहा जाए, नगर के मसान होने में क्या कमी रह गई?”
दिल्ली से वृंदावन आगमन के कारणों में ग़दर तो था ही, लेकिन रसखान ने प्रेमवाटिका में इस संबंध में किसी मानिनी के मान से आहत होने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि “तोरि मानिनी तें हियो, फोरि मोहिनी-मान। / प्रेम देव की छविहि लखि, भए मियाँ रसखान॥” अर्थात् मानिनी से हृदय से तोड़कर, उसका मान भंगकर प्रेमदेव कृष्ण की छवि देखी, जिससे मिया रसखान हो गए। यह अंतः साक्ष्य है, इसलिए विश्वसनीय प्रतीत होता है। ज़ाहिर है, रसखान किसी सुंदर स्त्री से प्रेम करते थे, लेकिन वह मानिनी थी, इसलिए रसखान उससे विरक्त होकर कृष्ण की ओर आकृष्ट हुए। लगता है इसी उल्लेख का रूपांतरित प्रकरण ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ और रसखान के संबंध में प्रचलित जनश्रुतियों में आया है। ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में उल्लेख है कि रसखान दिल्ली के किसी साहूकार के सुंदर पुत्र पर अनुरक्त थे। रसखान ने चार वैष्णवों को भगवतवार्ता करते हुए सुना कि प्रभु में चित्त इस तरह लगाना चाहिए जैसे रसखान ने साहूकार के बेटे से लगाया है। रसखान ने जब उनसे प्रभु के स्वरूप के संबंध में पूछा, तो वैष्णवों ने उन्हें श्रीनाथजी का चित्र दिखाया। रसखान उस पर मुग्ध होकर वृंदावन गए और वेश बदलकर मंदिरों में दर्शन करने लगे। गोपालपुरा में उनको पुजारी ने धक्का दिया, जिससे वे गोविंदकुंड में जा गिरे। स्वयं श्रीनाथजी ने रसखान को दर्शन दिए। उन्होंने विट्ठलनाथ को आदेश दिया कि वे रसखान को दीक्षा दे। राधाचरण गोस्वामी के अनुसार, वे कृष्ण का चित्र देखकर उस पर मुग्ध हो गए और वृंदावन चले आए। रसखान के संबंध में प्रचलित दो जनश्रुतियाँ भी लगती है, प्रेमवाटिका के अंतःसाक्ष्य का रूपांतर हैं। पहली जनश्रुति के अनुसार, कहीं श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी। रसखान भी कथा सुनने बैठ गए। उन्होंने कथावाचक से कृष्ण के संबंध में पूछा, तो उसने कहा कि ये रस की खान कृष्ण हैं। रसखान कृष्ण पर ऐसे मुग्ध हुए कि वे वृंदावन चले गए और अपना नामकरण भी 'रसखान' कर लिया। दूसरी जनश्रुति के अनुसार, वे अपने साथियों के साथ हज करने मक्का की यात्रा पर निकले, लेकिन मार्ग में वृंदावन में कृष्ण का स्वरूप देखकर वे उसमें ही रम गए। कहते हैं कि बाद में लोगों ने बादशाह से इसकी शिकायत की, जिससे रसखान आहत हुए। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दोहे में अपनी यह पीड़ा व्यक्त की है। वे कहते हैं—
कहा करै रसखानि को, को चुगुल लबार।
जो पै राखनहार हे, माखन चाखनहार॥
अर्थात् जो यदि माखन चखने वाले कृष्ण रक्षक हैं, तो कोई चुग़लख़ोर और झूठा, रसखान का क्या कर सकता है?
रसखान गोस्वामी विठ्ठलनाथ के दीक्षित शिष्य थे। वृंदावन जाकर रसखान वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ (1515-1585 ई.) के शिष्य हो गए, यह उल्लेख दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में (1695 ई.) वल्लभाचार्य के 84 और दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता में उनके पुत्र विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। वार्ता ग्रंथों की प्रमाणिकता आरंभ में उसके साथ गोकुलनाथ (1551-1610 ई.) और हरिराय (1540-1715 ई.) के दो नाम संबद्ध होने के कारण संदिग्ध मानी जाती थी, लेकिन अब उस संबंध में भ्रम दूर हुआ है। वार्ताओं का विकास क्रमशः हुआ, लेकिन परवर्ती वार्ताओं में कोशिश यह की गई कि उनके विस्तार को रचना के मूल से अलग रखा जाए। गोकुलनाथ कथित वार्ताओं को पहले कृष्ण भट्ट और फिर हरिराय ने संकलित-संपादित किया। फ़िलहाल उपलब्ध वार्ताएँ हरिराय द्वारा संकलित-संपादित हैं। उल्लेखनीय यह है कि मूल वार्ताकार गोकुलनाथ और रसखान के समय में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए इनको संदिग्ध मानने का कोई कारण नहीं है। यह अवश्य है कि मूल प्रकरण का वल्लभ संप्रदाय के अनुसार अनुकूलीकरण हुआ है। ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में उल्लेख है कि “...फेर श्रीनाथजी ने गुसाईं जी से कही ये जीव दैवी है। और म्लेच्छ योनि कुं पायौ है। जासुं याके ऊपर कृपा करो याकुं शरण लेउ॥ जहाँ सूधी तुमारो संबंध जीव कुं नहीं होवे तहाँ सूधी में वहा जीव को स्पर्श नहीं करहुं और वासुं बोलु नहीं हूँ। और वाके हाथ को खावहुँ नहीं जासुं आप याको अंगीकार करो। तब श्री गुसाईं श्रीनाथजी के वचन सुनकर गोविंदकुंड पधारे और वाकुं नाम सुनाए॥ और श्रीनाथजी दर्शन गुसाईंजी के स्वरूप में वाकुं भए॥ तब श्री गुसाईजी विनकुं संग लेके पधारे और उत्थापन के दर्शन कराए। महाप्रसाद लिवायो। तब रसखानजी श्रीनाथजी के स्वरूप में आसक्त भये॥ तब वे रसखान ने अनेक कीर्तन और कवित्त दोहा बहोत प्रकार बनाए। जैसे-जैसे लीला के दर्शन विनकुं भये। वैसे ही वर्णन किए। सो वे रसखान श्रीगुसाई जी के ऐसे कृपापात्र हते। जिनका चित्र के दर्शन करत मात्र से ही संसार में से चित्त खेंचाय और श्रीनाथजी में लग्यो। इनके भाग्य की कहा बढ़ाई करनी॥” विट्ठलनाथ और रसखान लगभग समकालीन थे, इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि वे एक-दूसरे के संपर्क में आए होंगे। विट्ठलनाथ का प्रभाव और वर्चस्व वल्लभाचार्य की तुलना में अधिक था और उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को सांगठनिक स्वरूप दिया और पूजा-विधान आदि भी तय किए। अकबर से भी उनके संबंध अच्छे थे, इसलिए रसखान द्वारा उनसे दीक्षा लेने की बात सर्वथा निराधार भी नहीं कही जा सकती है। विट्ठलनाथ ने आग्रहपूर्वक संप्रदाय के विस्तार और वर्चस्व में दिलचस्पी ली थी, इसलिए संभावना है कि उन्होंने अपने संप्रदाय की लोकप्रियता के लिए बादशाह वंश के रसखान को अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद की, ऐसा हो सकता है।
रसखान का संबध तीन स्थानों—दिल्ली, पिहानी और वृंदावन से जोड़ा जाता है। दिल्ली और वृंदावन से उनका संबंध तो निर्विवाद है। दिल्ली में वे बादशाह वंश की ठसक के साथ जीवन के आरंभिक वर्षों में रहे। यह उल्लेख प्रेमवाटिका में मिलता है। उन्होंने लिखा है कि “देखि गदर हित साहबी, दिल्ली नगर मसान। / छिनहिं बादसा-बंस की, ठसक छोरि रसखान॥” अर्थात् बादशाहत के लिए हुए ग़दर से दिल्ली नगर श्मशान हो गया और रसखान ने क्षण भर में ही बादशाह वंश की ठसक छोड़ दी। प्रेमवाटिका में ही यह उल्लेख भी है कि उनके जीवन का शेष अधिकांश समय वृंदावन में कृष्णभक्ति में व्यतीत हुआ। उन्होंने लिखा है कि “प्रेम निकेतन श्रीबनहि, आइ गोवर्धन धाम। / लह्यौ सरन चित चाहिकै, जुगल सरूप ललाम॥” अर्थात् प्रेम के निवास स्थान वृंदावन आया और युगलस्वरूप सुंदर भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ली। संभवतः इसी आधार पर राधाचरण गोस्वामी ने भी उनको दिल्ली का ही निवासी माना है। उन्होंने लिखा है कि “दिल्ली नगर निवास बादसा बंस-बिभाकर।” अर्थात् दिल्ली नगर के निवासी और बादशाह वंश के सूर्य थे। विद्वानों का एक वर्ग पिहानी (हरदोई, उत्तर प्रदेश) को उनका जन्मस्थान मानता है। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में उनके आगे ‘पिहानेवाले’ लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, पिहानी में सैयद पठानों की बस्ती है और संभवतः दिल्ली में पठानों के शासनकाल के दौरान उनके माता-पिता दिल्ली आ गए होंगे। माजदा असद की धारणा इससे अलग है। उनका मानना है कि सैयद और पठान मुसलमानों की दो अलग उपजातियाँ हैं। उनकी इस धारणा के आधार पर कुछ विद्वान् उनको सैयदवंशीय ठहराकर उनका जन्म पिहानी में मानते हैं। यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि शेरशाह सूरि द्वारा पीछा किए जाने पर हुमायूँ को कन्नौज के क़ाज़ी सैयद अब्दुल ग़फ़ूर ने आश्रय दिया था। हमायूँ ने बाद में उसे हरदोई ज़िले की शाहाबद तहसील में 500 बीघा जंगल और पाँच गाँव दिए थे। शायद रसखान इसी सैयद वंश से संबंधित रहे हों। रसखान का निधन 1628 ई. के आसपास मथुरा-वृंदावन में हुआ। महावन में उनका समाधि-स्थल आज भी है।
तीन
रसखान का रचना संसार बहुत सीमित है और प्रेमवाटिका को छोड़कर उनकी शेष रचनाएँ अव्यवस्थित रूप में यहाँ-वहाँ मिलती हैं। प्रेमवाटिका उनकी सुनियोजित 53 दोहों की एक रचना है, अन्यथा उनकी कवित्त-सवैया रचनाएँ संगीतप्रधान रचनाओं के प्रसिद्ध संचयनों—रागरत्नाकर, वृहदरागरत्नाकर और रागकल्पद्रुम में प्रकीर्णक रूप में रागों के आधार पर संकलित मिलती हैं। उनकी कवित्त-सवैया रचनाओं के संकलन सुजान-रसखान का संचयन कब और किसने किया, यह ज्ञात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी दो रचनाओं—प्रेमवाटिका और सुजान-रसखान का ही उल्लेख किया है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रसखानशतक और पदावली शीर्षक वाली दो और रचनाओं का परिचय दिया है। रसखान की रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार उनके समय में अयोध्यासिंह उपाध्याय और जगनाथदास रत्नाकार और भारत कला-भवन, वाराणसी में उपलब्ध थीं। रसखान की रचना दानलीला म्युनिसिपल म्यूज़ियम इलाहाबाद में है। रसखान के कवित्त सवैये और भी कई संचयनों में उपलब्ध हैं। सबसे पहले उनकी रचनाओं का संकलन किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रेमवाटिका (1907 ई.) और सुजान-रसखान (1919 ई) के नाम से किया। बाद में उनके कई संचयन भी प्रकाशित हुए। सभी संचयन कमोबेश एक जैसे हैं—केवल इनमें एक-दो रचनाएँ कम या ज़्यादा हैं। अभी तक उपलब्ध रसखान की रचनाओं के संचयनों में सबसे अधिक प्रामाणिक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संचयन ‘रसखानि ग्रंथावाली’ (1953 ई.) को माना जाता है। रसखानि ग्रंथावली में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान की रचनाओं को चार उपशीर्षकों 'सुजान-रसखानि', 'दानलीला', 'प्रेमवाटिका' और 'प्रकीर्णक' में वर्गीकृत किया है। सुजान-रसखान की रचनाएँ कुछ विषय आधारित उपशीर्षकों—'बाललीला', 'गोचारण', 'चीरहरण', 'कुंजलीला', 'रासलीला', 'पनघटनीला', 'दानलीला', 'वंशी', 'वनलीला' आदि में वर्गीकृत हैं। उनकी कुछ अवर्गीकृत स्फुट रचनाएँ भी मिलती हैं। रसखान ने कृष्णलीला का ही नहीं, गंगा और शिव की महिमा का भी वर्णन किया है। उनकी गंगामहिमा की दो और शिवमहिमा की एक रचना मिलती हैं। रसखान के 26 दोहे 'अष्टयाम' के शीर्षक से कल्याण (1955 ई.) के 'संतवाणी अंक' में प्रकाशित हुए थे। इनमें से कुछ दोहे सुजान-रसखान में सम्मिलित हैं। वैसे ब्रजभाषा में अष्टयाम काव्य की परंपरा है, लेकिन विद्वान् इसके प्राप्ति स्रोत की सूचना की अनुपलब्धता के कारण इनकी प्रामाणिकता के संबंध में बहुत आश्वस्त नहीं हैं।
चार
रसखान ने अपने प्रेम के आदर्श का अलग से प्रेमवाटिका में वर्णन किया है। प्रेम का यह आदर्श लिया-दिया गया आदर्श नहीं है। यह उनका अपना आदर्श है, जो उन्होंने अपने जीवनानुभवों और सत्संग से अर्जित किया है। ऐसा नहीं हैं कि यदि है कि यह सर्वथा नया और पहली बार प्रस्तुत आदर्श है। प्रेम संबंधी उनके विचार भारतीय और सुफ़ी दार्शनिक विचारों से मिलते-जुलते हैं, लेकिन उनके प्रेम के आदर्श पर उनकी अपनी छाप है। रसखान वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसकी संभावना है, लेकिन उनका प्रेम का आदर्श वल्लभाचार्य के प्रेम के आदर्श से कुछ हद तक अलग है। वल्लभाचार्य का लक्ष्य भगवद्भक्ति और अलौकिक प्रेम है, लेकिन रसखान प्रेम में लौकिकता का तत्त्व भी आ गया है। रसखान ने प्रेम के सच्चे स्वरूप, लक्षण, भेद, व्यापकता और प्रभाव का अपने ढंग से वर्णन किया है। रसखान का सच्चा प्रेम यौवन और रूप पर निर्भर नहीं करता। यह कामनारहित और निःस्वार्थ है। उन्होंने प्रेमवाटिका में एक जगह लिखा है कि बिन गुन, जोबन, रूप, धन, बिन स्वारथ हित जानि॥ शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि॥ अर्थात् प्रेम गुण, यौवन, रूप, धन और स्वार्थ के बिना होता है। रसखान कहते हैं कि यह शुद्ध, संपूर्ण और कामनारहित होता है। रसखान ने प्रेम को एकरस और अहेतुक भी कहा है। वे एक जगह कहते हैं कि इक अंगी, बिनु कारनहि, इकरस सदा समान। / गर्ने प्रियहि सर्वस्व जो सोई प्रेम समान॥ अर्थात् प्रेम एकांगी, अकारण, एकरस और सदैव समान होता है। इसी तरह प्रेम प्रिय को सर्वस्व मानता है। रसखान की निगाह में प्रेम समस्त ज्ञान का कारण है। प्रेम को जान लेने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। उन्होंने इस संबंध में एक जगह कहा है कि जेहि बिनु जाने कछुहि नहिं, जानो जात विशेष। सोइ प्रेम जोहि जानि कै, रहि न जात कुछ शेष॥ अर्थात् प्रेम को जाने बिना कुछ भी नहीं है। लगता है जैसे कुछ विशेष नहीं जाना है। प्रेम ही है, जिसको जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। रसखान की निगाह में प्रेम सर्वोपरि और अलौकिक है। उनके अनुसार, प्रेम पा लेने के बाद ईश्वर और बैकुंठ की कामना नहीं रहती। एक जगह उन्होंने कहा है कि जोहि पाये बैकुंठ अरू हरिहू की नहीं चाहि।। सोइ अलौकिक शुद्ध शुभ सरस प्रेम कहाहि। अर्थात् जो बैकुंठ और ईश्वर की भी इच्छा नहीं करे, वही अलौकिक शुभ और सरस प्रेम कहलाता है। रसखान प्रेम को केवल दो मन की एकता तक सीमित नहीं रखते, वे इससे आगे दो शरीरों के ऐक्य तक जाते हैं। उन्होंने कहा है कि दो मन इक होते सुन्यो, पै वह प्रेम न आहि। / होहिं जबै द्वै तनहु इक सोई प्रेम कहाहि॥ अर्थात् प्रेम में दो मनों को एक होते सुना है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। जब दो शरीर एक होते हैं, वही प्रेम कहलाता है। रसखान की प्रेम मीमांसा पर शास्त्र का भी प्रभाव है। लगता है कि उन्होंने नारदपंचरात्र आदि प्रेम के सैद्धांतिक ग्रंथों का अनुशीलन किया था। उनके एकाधिक दोहों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि स्वारथमूल अशुद्ध ते, शुद्ध स्वाभावानुकूल। / नारदादि प्रस्तार करि, कियो जहि को तूल॥ अर्थात् स्वार्थप्रधान प्रेम अशुद्ध होता है और जो स्वभाव के अनुकूल सहज है, वह शुद्ध प्रेम है। नारद आदि ने इसी प्रेम की चर्चा विस्तार से की है। प्रेम का मार्ग रसखान के अनुसार बहुत सरल और सीधा भी है और बहुत कठिन और सूक्ष्म भी है। एक जगह उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि कमलतंतु से छीन अरू कठिन खड्ग की धार॥ अति सूधो टेंढ़ो बहुत प्रेम पंथ अनिवार। अर्थात् प्रेम का मार्ग कमलतंतु से क्षीण और खडूग की धार की तरह कठिन है। यह बहुत सीधा, टेढ़ा और अनिवार है।
पाँच
रसखान के यहाँ भक्ति का अर्थ कृष्ण से प्रेम है। कृष्ण उनके लक्ष्य, आलंबन आदि सब हैं। वे कृष्ण की अलौकिकता, सौंदर्य, लीला आदि का बहुत मनोयोग से वर्णन करते हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इतना अधिक है कि वे उनसे संबंधित वस्तुओं, प्राणियों और जगहों से भी प्रेम करते हैं। उनके अनुसार, जीवन की सार्थकता ही इसमें है कि यह कृष्ण से संबंधित वस्तुओं, प्राणियों और जगहों के सान्निध्य में व्यतीत हो। वे कहते हैं—
मानुस हाँ तो वही रसखान, बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मँझारन॥
पाहन हौं तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारन।
जो खग हौं तो बसेरो करौं मिलि कालिंदीकूल कदंब की डारन॥
अर्थात् रसखान कामना करते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जीवन मिले, तो मैं गोकुल के गाँव के ग्वालों के बीच निवास करूँ। यदि मुझे पशु जीवन मिले और बस चले, तो मैं नित्य नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। वे कहते मुझे पत्थर होना पड़े, तो मैं उस पहाड़ रूपी छत्र का होना चाहता हूँ, जो इंद्र से रक्षा के लिए कृष्ण ने धारण किया। जो मुझे पक्षी जीवन मिले, तो मेरी कामना है कि मेरा निवास यमुना नदी तट पर स्थित कदंब के वृक्ष की शाखाओं पर हो। कृष्ण उनके लिए अलौकिक लीलापुरुष हैं, जो मनुष्य के प्रेम के अधीन हैं। वे कहते हैं—
सेस गनेस महेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं।
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें।
नारद से सुक ब्यास रहैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं॥
अर्थात् शेषनाग, गणेश, शंकर और सूर्य, जिसका गुणगान करते हुए जिसे अनादि, अनंत, अखंड, अछेद्य और अभेद बताते हैं। नारद, सुकदेव और व्यास प्रयत्न करके हार गए, लेकिन जो उनका पार नहीं पा सके, उसी कृष्ण को अहीर कन्याएँ थोड़े से छाछ के लिए नृत्य करवाती हैं। कृष्ण के प्रति रसखान का समर्पण और प्रेम अनन्य है। कृष्ण ही उनका साधन और साध्य हैं। उन्होंने साफ़ कहा है कि कोऊ रमा भजि लेहु महाधन कोऊ कहूँ मन वांछित पावौ। / पै रसखानि वही मेरा साधन और त्रिलौक रहौ कि बसावौ॥ अर्थात् कोई लक्ष्मी की उपासना कर महाधन प्राप्त करे या कोई मनवांछित पल पाए, लेकिन मेरे तो साधन कृष्ण ही हैं, फिर चाहे मैं त्रिलोक और कहीं रहूँ या निवास करूँ।
राधा और कृष्ण के प्रेम में संयोग का उन्होंने बहुत ऐंद्रिक और मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने दो बँधे छवि प्रेम के बंधन के एकाधिक रूपों का वर्णन किया है। एक दुपहर में वे राधा और कृष्ण के संयोग का वर्णन करते हुए राधा के शब्दों में कहते हैं—
मोहिनी मोहन सों रसखानि अचानक भेंट भई बन माहीं।
जेठ की घाम भई सुखघाम आनंद हौ अंग ही अंग समाहीं।
जीवन को फल पायौ भटू रस-बातन केलि सों तोरत नाहीं।
कान्ह को हाथ कंधा पर है मुख ऊपर मोर किरीट की छाहीं॥
अर्थात् मोहिनी राधा की भेंट वन में मोहन कृष्ण से हुई। जेठ की धूप सुबह की धूप होकर दोनों के अंगों में आनंद की तरह समा गई। हे सखी! मुझे जीवन का आनंद मिल गया। रसपूर्ण बातें और केलि क्रीड़ाएँ ख़त्म ही नहीं हुईं। कृष्ण का हाथ मेरे कंधे पर है और मेरे मुख पर उनके मोर मुकुट की छाया है।
कृष्ण का बाल्य जीवन भी रसखान का वर्ण्य है। उन्होंने कृष्ण के बालरूप के सौंदर्य और उनकी मनोरम चेष्टाओं के कई चित्र खींचे हैं। कहीं माँ यशोदा उन्हें गाय की ओट में ढूँढ़ रही हैं (धेनु की ओठ ढिंढ़ोरत), कहीं उनके वस्त्र धूल में भरे हुए हैं (रज माँहि विथूरि दुकूलैं), कहीं उनको तेल लगाकर काजल से डिठौना बनाया गया है (तेल लगाइ लगाइ कै अँजन भौंहें बनाइ बनाइ डिठौनहिं), कहीं वे पैंजनिया और पीला कमरवस्त्र पहनकर खेलते और खाते हुए आँगन में घूम रहे हैं (खेलत खात फिरै अँगना पर पैंजनी बाजति पौरी कछौटी) और कहीं उनके हाथ से सौभाग्यवान् कौआ माखन-रोटी छीनकर ले गया है। (काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लै गयौ माखन रोटी)। रसखान कृष्ण के इस बालरूप पर करोड़ों कामकलाएँ न्यौछावर करते हैं। वे कहते हैं कि वा छबि को रसखानि बिलोकत वारत काम कला निज-कोटी।
कृष्ण के रूप-सौंदर्य पर रसखान अभिभूत और मुग्ध हैं। उन्होंने उनके अंग-प्रत्यंगों और आंगिक चेष्टाओं के स्वाभाविक सौंदर्य और उनके बाह्य श्रृंगार का मनोरम वर्णन किया है। कृष्ण के गले में शोभित माला और पगड़ी का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मोतिन लाल बनी नट के, लटकी लटवा लट घूँघरवारी। / अंग ही अंग जराव लसै अरु सीस लसै पगिया जरतारी। अर्थात् मोतियों की माला नटनागर कृष्ण के गले में सुशोभित है और उस पर उनके घुँघराले बालों की लटें लटकी हुई हैं। अंगों पर जड़ाऊ आभूषण सुशोभित हैं और सिर पर जरी की पगड़ी अच्छी लग रही है। कृष्ण की आँखों, मुख और मधुर वाणी का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि बाँको बड़ी अँखियाँ बड़रारे कपोलनि बोलनि कौं कल बानी। / सुंदर रासि सुधानिधि सो मुख मूरति रंग सुधारस-सानी। अर्थात् कृष्ण की आँखें वक्र, कपोल बड़े और वाणी बहुत मधुर है। उनका शरीर चंद्रमा है और यह अमृत से सना हुआ है। एक और जगह उनके कानों के कुंडल, सिर के मोरपंख और नए वस्त्र की सराहना करते हुए रसखान ने लिखा है कि दोउ कानन कुंडल मोरपखा सिर सोहै दुकूल नयो चटको॥ मनिहार गरे सुकुमार धरे नट-भेस अरे पिय को टटको। अर्थात् कृष्ण दोनों कानों में कुंडल, सिर पर मोरपंख और शरीर पर नया चटकीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। सुकुमार कृष्ण ने गले में मोतियों का हार धारण कर नटनागर वेश बना रखा है।
रसखान कृष्ण के रूप-सौंदर्य में सबसे अधिक उनकी 'बंक बिलोकनि' पर आसक्त हैं। कृष्ण की इस मुद्रा का वर्णन उन्होंने अपने कवित्त-सवैयों में कई तरह से किया है। एक सवैये में उन्होंने कहा है कि अबलोकन बंक बिलोचन मैं ब्रजबालन के दृग जोरत है। अर्थात् कृष्ण की वक्रदृष्टि ब्रजबालाओं के नेत्रों को सुख प्रदान करती है। एक और जगह वे कहते हैं कि दीरघ बंक बिलोकनि की अबलोकनि चोरति चित्त को चैना। अर्थात् दीर्घ नेत्रों की वक्र दृष्टि चित्त का चैन चोरी करती है। इसी तरह एक और जगह उन्होंने कहा है कि तिरछी बरछी सम मारत है दृग-बान कमान मुकान लग्यौ॥ अर्थात् कृष्ण के कानों तक फैले हुए दृग तिरछी बरछी की तरह मार करते हैं।
छः
रसखान की निगाह में कृष्ण लीलापुरुष हैं, इसलिए उन्होंने उनकी प्रेम, राग, फाग और दान लीलाओं का बहुत जीवंत और मनोरम वर्णन किया है। कृष्ण की प्रेमलीला के रसखान की कविता में कई रूप हैं। युमना में जल लेने जाती हुई गोपी से कृष्ण की प्रेमलीला का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं—
जात हुती जमुना जल कौं मनमोहन घेरि लयौ मग आइ कै।
मोद भर्यो लपटाइ लयौ पट घूँघट ढारि दयौ चित चाइ कै।
और कहा रसखानि कहौं मुख चूमत घातन बात बनाइ कै।
कैसे निभै कुल-कानि रही हिये साँवरी मूरति की छबि छाइ कै॥
अर्थात् एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं यमुना से पानी लेने जा रही थी कि मनमोहन कृष्ण ने आकर मुझे घेर लिया। आनंद से भरकर उसने मुझे अपने से लिपटाकर घूँघट हटा दिया। और क्या कहूँ? धोखे से बात बनाकर उसने मेरा मुँह चूम लिया। अब कुल की मर्यादा का निर्वहन कैसे हो? मेरे हृदय में उसकी साँवली मूर्ति की छवि छाई हुई है। एक और गोपी की विवशता के संबंध में रसखान कहते हैं कि माखी भई मधु की तरुनी बरुनीन के बान बिंधीं कित जाहीं। / बीथिन डोलति हैं रसखानि रहें निज मंदिर में पल नाहीं॥ वह तरुणी शहद की मक्खी की तरह बरौनियों के बाण से बँधी हुई और कहाँ जा सकती है? गलियों में रसखान कृष्ण डोल रहे हैं और उसे अपने घर में चैन नहीं है। कृष्ण की कुंज और फागलीला का वर्णन पारंपरिक है, लेकिन रसखान ने अपने वर्णन से उनमें प्राण डाल दिए हैं। कृष्ण की कुंजलीला का वर्णन करते हुए वे एक जगह कहते हैं कि कुंजगली मैं अली निकसी तहाँ साँकरे ढोटा कियौ भटभेरो। माई री वा मुख की मुस्कान गयौ मन बूढ़ि फिरै नहिं फेरो॥ अर्थात् हे सखी! मैं कुंज गली में निकली, जहाँ सँकरे मार्ग में मेरी मुठभेड़ कृष्ण से हो गई। हे सखी! उसकी मुस्कान में मेरा मन ऐसा डूबा कि अब मैं उससे उबर नहीं पा रही हूँ। फागलीला के रसखान के वर्णित दृश्य भी अद्भुत हैं। रसखान एक जगह एक गोपी के शब्दों में कहते हैं कि फागुन लाग्यौ सखि जब तें, तब तें ब्रजमंडल धूम मच्यौ है। नारि नवेली बचें नहिं एक बिसेख यहै सबै प्रेम अच्यौ है। अर्थात् जब से फाल्गुन लगा है तब से ब्रजमंडल में धूम मची हुई है। कोई नवेली स्त्री नहीं है जिसने प्रेम का आचमन न किया हो। रसखान की रासलीला का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तृत है। मुरली वट के नीचे कृष्ण द्वारा रचे गए रास के प्रभाव का विवरण रसखान के शब्दों में एक गोपी इस तरह देती है—
आजु भटू इक गोपकुमार ने रास रच्यौ इक गोप के द्वारे।
सुंदर बानिक सों रसखानि बन्यौ वह छोहरा भाग हमारे।
ए बिधना! जो हमैं हँसतीं अब नेकु कहूँ उतकों पग धारें।
ताहि बदौं फिरि आबे घरै बिनही तन औ मन जौवन बारें॥
अर्थात् आज गोपकुमार कृष्ण ने एक गोप के द्वार पर रास रचा। हमारा सौभाग्य है कि नंदपुत्र इसमें सबसे अच्छे वेशवाला बन गया। हे विधाता! मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि आज तक जो हमारे प्रेम पर हँसती हैं वे भी अपना मन और रूप-यौवन कृष्ण पर न्यौछावर किए बिना वापस नहीं आएँगी। रास में कृष्ण की बाँसुरी के गोपियों पर प्रभाव का वर्णन रसखान ने बहुत मनोयोग से किया है। एक जगह वे कहते हैं—
रसखान आज भटू इक गोपबंधू भई बावरी नेकु न अंग सम्हारै।
माई सु धाइ कै टौना सो ढूँढ़ति सास सयानी-सवानी पुकारै।
यौं रसखानि घिरौ सिगरौ ब्रज आन को आन उपाय बिचारै।
कोउ न कान्हघर के कर ते वहि बैरिनि बाँसरिया गाहि जारै॥
अर्थात् हे सखी! आज एक गोपवधू बाँसुरी की धुन सुनकर पागल हो गई है। उसे अपने अंगों को सँभालने का तनिक भी ध्यान नहीं है। उसकी सखियाँ जादू करने वालों को ढूँढ़ रही हैं। उसकी सास सयानों को बुला रही है। इस तरह ब्रज घिर गया और लोग अन्य उपाय करने पर विचार कर रहे हैं। कोई कृष्ण की इस बाँसुरी को जला क्यों नहीं देता!
'दानलीला' कृष्णभक्त कवियों की अद्भुत कल्पना है। दान का अर्थ 'कर' है—कृष्ण अपने को स्वयंभू अधिकारी मानकर दूध-दही बेचने जाने वाली गोपियों से कर माँगने का अभिनय करते हैं। कर तो बहाना है—कृष्ण की कामना तो गोपियों से प्रेम पाने की है। रसखान ने दानलीला में विशेष रुचि ली है। उनकी दानलीला नाम से कवित-सवैया की एक छोटी-सी अलग रचना मिलती है। दानलीला दरअसल राधा-गोपियों और कृष्ण के बीच दान को लेकर लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में होनेवाला रोचक संवाद है। गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि “आवत हौ रस के चसके तुम जानत हौ रस होत कहा हो। / नैसुक वै रस भीजन दैहौ दिना दस के अलबेले लला हो।” अर्थात् जिस रस की इच्छा से तुम हमारे पास आते हो, तुम्हें नहीं पता कि वह रस होता क्या है? थोड़ा अभी उस रस से अपने को भीगने दो। अभी तो तुम दस दिन अर्थात् अल्पायु बालक हो। कृष्ण दूध-दही बेचने के लिए जाने वाली राधा से कहते हैं कि “आई हौ आज नई ब्रज में कछु नैन नचाइ के रार मचैहौ। / बानति हौ हमहीं छलि कै दधि बेचन जाव सो जान न पैहौ।” अर्थात् तुम आज ब्रज नई आई हो, इसलिए आँखें नचाकर झगड़ा कर रही हो। कुछ भी करो हमें छलकर तुम दही बेचने नहीं जा सकतीं। राधा उत्तर में कहती है—
सुनिकै यह बात हियें गुनि कै तब बोलि उठि वृषभान-लली।
कहौ कान्ह अजान भए बन में कहूँ माँगत दान कि छेकि गली।
मग आइ कै जाइ रिसाइ कहा तुम एकऊ बात कही न भली।
हम हैं वृषभानपुरा की लली अब गोरस बेचन जात चली॥
अर्थात् यह सुनकर अपने हृदय में विचार करती हुई वृषभानुकुमारी राधा कहती है कि क्यों अनजान बनकर, रास्ता रोककर दान माँगते हो? मार्ग में आकर क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? तुमने एक भी बात अच्छी नहीं कही। मैं वृषभानुकुमारी हूँ और दूध बेचने के लिए जा रही हूँ।
सात
रसखान आग्रहपूर्वक कवि नहीं, भक्त हैं, लेकिन परंपरा से प्राप्त कवित्त-सवैया की ब्रजभाषा परंपरा का सघन निवेश उनकी कविता में है। वे ठेठ और खाँटी ब्रजभाषा के कवि हैं। उन्हें इसमें अनायास महारत हासिल है। उनकी कविता की सबसे बड़ी ख़ासियत उसकी अनायास आनुप्रासिक वर्णयोजना और शब्द चयन है। उनकी कविता में इस कारण लय और सांगितिकता आ गई है। “आवत लाल गुलाल लिए मग सूने मिलो इक नार नवेली”, “मोतिन लाल बनी नट के लटकी लटवा लट घूँघरवारी” और “अलबेली बिलोकनि बोलनि औ अलबेलियै लोल निहारन” जैसी पंक्तियों में जो आनुप्रासिकता और शब्दयोजना है, वह कमोबेश उनकी सभी रचनाओं में हैं। रसखान के अप्रस्तुतविधान में अलंकरण आदि का तामझाम और आडंबर नहीं है। दरअसल उनकी सहजोक्तियाँ ही कविता बन गई हैं। कामदेव, रति, चंद्रमा, तारे, बाण आदि रसखान के प्रिय उपमान और प्रतीक हैं। परंपरा से ब्रज में इनका प्रयोग होता आया है और रसखान भी इनका प्रयोग ख़ूब करते हैं। श्लिष्ट प्रयोग रसखान ने नहीं किए हैं, पर अपने उपनाम 'रसखान' का उन्होंने यमक और श्लेष प्रयोग जमकर किया है। शब्दों के माध्यम से चित्रों की योजना रसखान के यहाँ ख़ूब है और यह उनकी कविता की विशेषता भी है। तुलसीबन में निकले श्रीकृष्ण का एक चित्र रसखान ने उस तरह गढ़ा है—
आजु री नंदलला निकस्यौ तुलसीबन तें बन कैं मुसकातो।
देखें बनै न बनै कहतै अब सो सुख जो मुख मैं न समातो।
हौं रसखानि बिलोकिबे कौं कुलकानि के काज कियौ हिय हातो।
आइ गई अलबेली अचानक ए भटू लाज को काज कहा तो॥
अर्थात् आज बन-ठनकर नंदपुत्र कृष्ण तुलसी वन से निकला। उसकी शोभा न देखते बनती है और न कहते ही बनती है और उसे देखकर जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन संभव ही नहीं है। उसको देखने के लिए ब्रजबालाओं ने कुलमर्यादाएँ छोड़ दी हैं। इतने में एक और अलबेली बाला आ गई। हे सखी। फिर क्या था, सभी ने अपनी लज्जा भी छोड़ दी।
रसखान की अधिकांश जीवनयात्रा अनुमानों पर आधारित हैं। उनके वृंदावनपूर्व जीवन के संबंध में कोई साक्ष्य और लोकस्मृति नहीं है। केवल कुछ अंतः, बाह्य और पारिस्थितिकीय साक्ष्यों के आधार उनके जीवन की कल्पना की जा सकती है। यह तो तय है कि वे वृंदावन में रहे और कृष्णभक्त कवि थे। उनका जन्म संभवतः सैयद या पठान परिवार 1533 ई. के आसपास हुआ। दिल्ली में 1554 से 1557 ई. में ग़दर जैसी स्थिति हो जाने और किसी सुंदर स्त्री के मान से आहत और विरक्त होकर वे वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुँचने के एक-दो वर्षों के दौरान विट्ठलनाथ के संपर्क में आए और इसी समय संभवतः उन्होंने उनसे दीक्षा ली। वेणीमाधवदास के उल्लेख के अनुसार, वृंदावन में रहते हुए संभवतः उन्होंने 1560-65 ई. के बीच कभी रामचरितमानस सुनी। जीवन के उत्तरार्ध, 90-91 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रेमवाटिका की रचना की और संभवतः 1628 ई. के आसपास उनका निधन हो गया। रसखान मुसलमान थे, लेकिन का जैसा उनका कृष्णप्रेम और जैसी उनकी ठेठ-खाँटी ब्रजभाषा है, उससे कुछ लोगों को यह संदेह करने का आधार मिल गया है कि उनकी रचनाएँ उनकी अपनी नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि रसखान सैयद इब्राहिम से अलग कोई और रसखान है। रसखान सदियों से ब्रजमंडल की लोकस्मृति में हैं, उनका समाधि स्थल भी है और उनके समय के आसपास के भगवत रसिक और गोकुलनाथ-हरिराय ने अपनी रचनाओं में उनका कृष्णभक्त-कवि के रूप में स्मरण भी किया है, इसलिए उनके ऐतिहासिक अस्तित्व और उनकी कविता की प्रामाणिकता पर संदेह का यह कोई बहुत युक्तिसंगत आधार नहीं है।
रसखान की कविता की विषय-वस्तु बहुत सीमित है। केवल कृष्ण उनके आलंबन हैं, लेकिन इससे जुड़े जितने विविध विषयों—कृष्ण का सौंदर्य, राधा का सौंदर्य, प्रेमलीला, रासलीला फागलीला, दानलीला, नेत्रोपालंभ, विरह, संयोग, मुरली, सखी, शिक्षा आदि का जो विधान रसखान ने किया है, वह आश्चर्यजनक है। रसखान ने जो भी कहा, कृष्ण, राधा और गोपियों का कहा, लेकिन यह सब उनका अपना है। वे केवल माध्यम नहीं हैं—वे कृष्ण, राधा और गोपियों के चित्त में गहरे उतरकर उनके जैसे बन गए हैं। प्रेम में कृष्ण, राधा और गोपियों की अंतः और बाह्य वृत्तियों की जैसी समझ उनको है, वह कम कृष्णभक्त कवियों के यहाँ मिलती है। रसखान के वृंदावनपूर्व जीवन के जो सांकेतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनसे लगता है कि वे वृंदावन में वैभव को देखकर और उससे गुजरकर आए थे। उन्होंने प्रेमवाटिका में बादशाही ठसक छोड़कर वृंदावन आने की ओर संकेत किया है। सुजान-रसखान में उनके वैयक्तिक जीवन के संबंध में कोई संकेत नहीं मिलता है, लेकिन इसमें उनका वैभव के प्रति वितृष्णा का भाव तो कई जगह दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपने एक सवैये में साफ़ लिखा है कि—“कोटिक ये कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारौं॥” अर्थात् करोड़ों सोने-चाँदी के भवन मैं वृंदावन के करील के कुंजों पर न्यौछावर करता हूँ। मुसलमान होते हुए भी रसखान का कृष्णभक्ति की ओर प्रवृत्त होना आश्चर्यजनक है, लेकिन लगता है कि मध्यकाल में मुसलमान और हिंदू धर्मों-समाजों में दीवारें बहुत बड़ी और अलंघ्य नहीं थीं और शायद एक मुसलमान का रसखान होना संभव और मान्य रहा होगा।
- पुस्तक : कालजयी कवि और उनका काव्य रसखान (पृष्ठ 5)
- संपादक : माधव हाड़ा
- रचनाकार : माधव हाड़ा
- प्रकाशन : राजपाल एण्ड सन्ज़
- संस्करण : 2025
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.