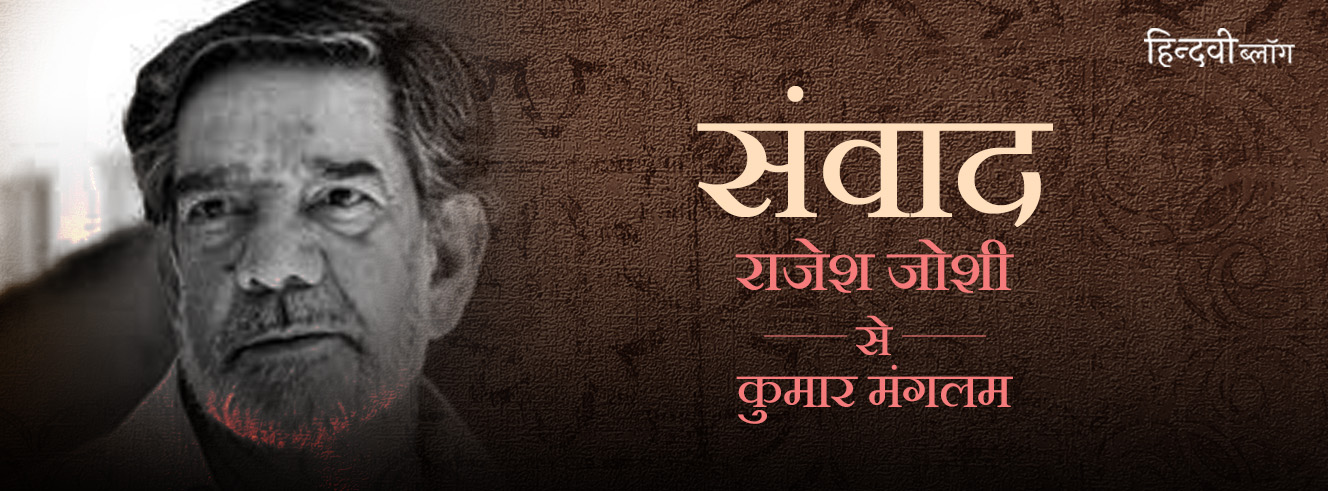
नई कविता नई पीढ़ी ही नहीं बनाती
 कुमार मंगलम
04 अक्तूबर 2023
कुमार मंगलम
04 अक्तूबर 2023
समय की समझदारी का चेहरा तत्कालीन पीढ़ियों के कई सारे लोग मिल कर बनाते हैं। समकालीन कविता के महत्त्वपूर्ण कवि-लेखक राजेश जोशी से उनकी रचनाओं के आस-पास या यूँ कहें उनके रचना-समय के आस-पास पिछले दिनों एक व्यवस्थित-सी अव्यवस्थित बातचीत संभव हुई। व्यवस्थित इसलिए कि यह बातचीत नियत थी और इसका अंततः यह औपचारिक रूप सामने है, और अव्यवस्थित इसलिए कि इसमें ख़ास आग्रह और सुनियोजित सवाल नहीं रखे गए। कोशिश यही रही की बातचीत को साक्षात्कार की शक्ल में नहीं रखा जाए, बहुत हद तक इसमें बातचीत की एक सहज लय मौजूद रहे, सवालों का क्रम भी बातचीत से ही निकलता रहे, जिसके केंद्र में समकालीनता और कविता का शहर ही प्रमुखता से विन्यस्त हो। राजेश जोशी अनौपचारिक बातचीत में बेहद सहज और बेलाग रहते हैं। उनकी चिंताएँ और सरोकार बेहद स्पष्टता और पक्षधरता के साथ उनके लिखे में हिंदी का व्यापक लोकवृत्त समझता रहा है, लेकिन बातचीत की इस औपचारिकता में उनका कवि-चिंतक और आलोचक रूप भी सजगता से अभिव्यक्त हो, इसका ख़ास ख़याल रखा गया है। यह बातचीत किसी बंधन में नहीं है। यहाँ स्मृतियों की उड़ान है और एक बहक भी। सवालों की केंद्रीयता के लिहाज़ से उन्हें थोड़ा संपादित कर दिया गया है। कोशिश यही है कि वाक्य-संरचना को बातचीत की शक्ल में ही रखा जाए।
— कुमार मंगलम
देखिए, यह एक बड़ी बहस है। कविता का शहर वाली किताब में भी इसे मैंने लिया है। सुरिंदर एस. जोढका का लेख है : ‘नेशन एंड विलेज, इमेज ऑफ़ रूरल इंडिया : गांधी नेहरू एंड अंबेडकर’। इसके अलावा भी अनेक लेख इस विषय पर लिखे गए हैं। यह एक बड़ी बहस है। गांधी ने भी गाँव को लेकर अपनी अवधारणाओं में बाद में बदलाव किए। यूँ देखें तो भारतीय समाज में सिर्फ़ दो ही समाज थे—नगरीय समाज था और दूसरा आरण्यक समाज था। ग्रामीण समाज नहीं था। ग्रामीण समाज तो तब आता है, जब खेती-बाड़ी की शुरूआत होती है।
आप संस्कृत साहित्य को देखिए या पौराणिक-साहित्य देखिए, उसमें नगरीय समाज है और आरण्यक समाज है। कालिदास के यहाँ भी आरण्यक समाज है या नगर है। नगर राजधानी होते थे, व्यापारिक नगर होते थे। गाँव नहीं थे। जब गाँव समाज बन गया तो उसका तेज़ी से विस्तार हुआ, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ । नेहरू ने अपने लेखों में और गांधी जी को लिखे पत्रों में भी बार-बार यह माना कि गाँव सामंती व्यवस्था के सबसे भयानक केंद्र थे। उन्होंने कहा कि सामंतशाही अपना जीवन जी चुकी है। उनका यह भी विचार रहा है कि सामंतशाही ब्रिटिश राज से आर्गेनिक रूप से जुड़ी हुई है, और वह पतित है। इसलिए उनका विचार था कि गाँवों का नगरीकरण ज़रूरी है। भारतीय समाज की यथास्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि गाँव का विकास नहीं होने दिया गया। आज भी लाखों की संख्या में गाँव हैं। बहुत छोटे-छोटे गाँव हैं। मध्य प्रदेश में ही लगभग चौबीस हज़ार से ज़्यादा गाँव हैं। विकास की अवधारणा में ही बुनियादी खोट है। गाँव को जोड़कर नगर बनाए जाना चाहिए। अंबेडकर ने तो भारतीय गाँवों को नाबदान कहा है। जिसमें श्रम करने वाला दलित वर्ग गाँव की परिधि पर रहता है और सवर्ण वर्ग मुख्य गाँव में रहता है। गाँव आज भी सामंती जकड़न के शिकार हैं।
आज भी हम सुनते हैं कि फलाँ दलित ने चप्पल पहन ली तो उसको मार डाला। घोड़ी पर चढ़ गया तो मार डाला। शादी कर रहा है तो मार दिया। यह जो वर्णवादी और जातिवादी क्रूरताएँ और घटियापन हैं, उसका कारण गाँव की स्थितियों से जुड़ा है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, और अगर हैं तो उन पर वर्चस्वशाली सवर्ण समाज का क़ब्ज़ा है। इसलिए शहरीकरण तो यानी किसी भी सभ्य समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। शुरुआत में गांधी ने शहर की तीखी आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शहर की इमारत का निर्माण जिस सीमेंट से होता है, वह गाँव के रक्त से बनाया जाता है। बाद के दिनों में लेकिन गांधी का विचार बदला और उन्होंने विकसित गाँव की जो तस्वीर रखी, वह लगभग शहर जैसी ही थी। तो बिना नगरीकरण के कोई भी सभ्य समाज नहीं बन सकता। चीन ने अपने सारे गाँव इतने विकसित कर लिए हैं कि वहाँ पर वे सारी सुविधाएँ हैं जो शहरों में होती है। यह एक हद तक कहा जा सकता है कि अब सारा कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। लेकिन हमारे समाज की जो संरचना है, उसमें विकास की सारी सुविधाएँ नगर केंद्रित हैं। हमारी सरकारें न केवल गाँवों का शोषण करती हैं, वहाँ चेतना को विकसित नहीं होने दे रही।
इस नगरीकरण पर एक बात और कि जब अज्ञेय कहते हैं कि अमूमन शहरों को देखने का नज़रिया यह है—‘साँप तुम सभ्य तो नहीं हुए नहीं…’ उसको क्रिटिसाइज किया है आपने। गाँव को जब देखते हैं तो ‘भारत-माता ग्रामवासिनी’ वाली छवि भी है। शहर और गाँव की एक बायनरी बनती है तो क्या शहर और गाँव में कोई अंतर्सूत्र तलाशे जा सकते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे के विलोम न प्रतीत हों?
इस बायनरी का सबसे बड़ा कारण गाँव और शहर के बारे में गांधियन डिस्कोर्स है। गांधीवादी विचार था कि शहर पश्चिमी सभ्यता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक है। यह न केवल ग़लत अवधारणा थी, बल्कि गांधीवादी विचार की भी एक ग़लत व्याख्या थी। इसी से वह बायनरी बनती चली गई। इसलिए यह अभी तक कुछ जगहों पर हमें दिखाई देता है। मैं एक बात पूछता हूँ कि पूरे हिंदी साहित्य में जिस ढंग से प्रेमचंद गाँव को देखते हैं, जिस तरह प्रेमचंद गाँव के अंतर्विरोधों और विडंबनाओं को देखते हैं, गाँवों की जहालत को देखते हैं, जिस तरह ‘ठाकुर का कुआँ’ में जमींदारों के अत्याचारों को देखते हैं, आप हिंदी में एक कविता ढूँढ़कर बता सकते हैं जो गाँव के अंतर्विरोधों पर, सामंती अत्याचारों पर बात करती हो। जब गाँव आता है तो ‘भारत-माता ग्रामवासिनी’ आ जाता है। ‘अहा ग्राम्य जीवन’ जैसी कविता हमारे सामने आती है।
प्रेमचंद उसी समय में लिख रहे हैं, जिस समय में मैथिलीशरण गुप्त हैं, उसी समय प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है वह गाँव जो प्रेमचंद को दिख रहा है। तो गद्य में तो दिख रहा है, कविता में नहीं दिख रहा है। तो हिंदी कविता में गाँव वास्तव में, लगभग है ही नहीं। अक्सर काल्पनिक गाँव हैं। आदर्श गाँव की छवियाँ हैं। प्रेमचंद गाँवों के अंतर्विरोधों को देख रहे थे। जातिवाद को देख रहे थे, जमींदारों के अत्याचारों को देख रहे थे। उनकी राजनीतिक चेतना किस स्तर की है यह देख रहे थे, किस तरह की छुआछूत है, जातिवाद है… यह सब देख रहे थे। लेकिन कविता में क्यों नहीं है, अगर कहीं-कहीं है भी तो बहुत कम ही है।
दो बातें इससे निकलती हैं, एक तो यह कि ब्रेष्ट-लुकाच की एक बहस है—यथार्थवाद को लेकर और दूसरी कई बार क्या होता है कि कुछ रचनाएँ संकेत में कहती हैं। इस तुलना में कथा में ज़्यादा स्पेस होता है तो कथाकार बहुत डिटेलिंग के साथ इन सब चीज़ों को दर्ज करता चलता है। क्या कविता में ऐसा नहीं हुआ है कि गाँव के उस यथार्थ को संकेतों में भी दर्ज किया गया हो?
सियारामशरण गुप्त की एक अद्भुत कविता है—‘एक फूल की चाह’। देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दो। वह शूद्र लड़की है। बच्ची है, जो बीमारी से तप रही है। वह अपने पिता से कहती है कि देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो और वह बेचारा पिता है जो अपनी बेटी के मोह में मंदिर जाता है और मारा जाता है, क्योंकि वह मंदिर में घुसने की कोशिश करता है। गांधी जी का जो हरिजनों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन था, उस पर अगर कोई हिंदी साहित्य में एकमात्र अच्छी कविता ढूँढ़ना हो तो वह अकेली कविता है—‘एक फूल की चाह’—सियारामशरण गुप्त की। पंत जी की कविता है, जिसमें एक गाय की आँखों से किसान के घर पर जमींदार के ग़ुंडों के द्वारा किए गए हमले को देखा गया है। पंत जी की ‘भारत-माता ग्रामवासिनी’ भी है। उसमें भी हमारे समाज की उदासी और निर्धनता है। लेकिन ऐसी कविताओं को ढूँढ़ना पड़ता है। गद्य के साथ यह समस्या नहीं है। सवाल यह नहीं है कि गद्य में स्पेस ज़्यादा है और कविता संकेतों में बात करती है। विधाओं की अपनी सीमाएँ होती हैं तो अपनी शक्ति भी होती है। गद्य से हमको हमारे समाज की जो जानकारी मिलती है, अगर हम उसे नहीं पढ़ें तो कविता से हम भारतीय गाँव की हालत को नहीं जान सकते। भारतीय गाँव को जानने के लिये या तो हमें श्यामाचरण दुबे के पास या एम. श्रीनिवासन के पास जाना पड़ेगा या प्रेमचंद के पास जाना पड़ेगा।
मैं तो कवि हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी कविता में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देश का विभाजन हुआ, आप बताइए कोई कविता? कोई कविता नहीं है। ग्यारह कविताएँ अज्ञेय ने लिखीं। मैंने उस पर एक लेख लिखा था, ‘पूर्वग्रह’ में छपा है। तो विभाजन पर वे ही कविताएँ हैं, सिर्फ़ वे ग्यारह कविताएँ। वे बहुत अच्छी कविताएँ नहीं हैं। अज्ञेय की अच्छी कविताओं में उनकी गिनती नहीं है। लोग जानते तक नहीं है कि उन्होंने ऐसी कविताएँ लिखीं। उनकी एक कहानी है विभाजन पर—‘शरणार्थी’। वह कहानी तो फिर भी याद रहती है, कविताएँ किसी को याद नहीं रहतीं। बाबा नागार्जुन बिहार में बैठे हैं और अगर महाराष्ट्र में कोई घटना हो रही है तो भी वह कविता लिखते हैं। महत्त्वपूर्ण गद्य लिखा गया। ‘तमस’ जैसा उपन्यास लिखा गया, ‘झूठा-सच’ लिखा गया। उर्दू में लिखा गया। पंजाबी में लिखा गया। लेकिन विभाजन जैसी त्रासद घटना पर हिंदी कविता चुप है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि हिंदी कविता की इन प्रॉब्लम्स पर बात वैसे नहीं हुई है। जबकि हिंदी कविता में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हिंदी कविता चूक गई है।
कविता का शहर लोक के विरुद्ध या समानांतर स्थापित की गई अवधारणा है?
नहीं, लोक की जो अवधारणा है; वह लोगों ने सीमित कर दी। लोक सिर्फ़ गाँव नहीं है, जैसा मान लिया गया है। हमारे यहाँ लोक शब्द में पूरा विश्व है। लोक-परलोक। उसमें सब कुछ लोक है। यह मान लेना कि सिर्फ़ ग्रामीण लोक ही लोक है और शहरी लोक, लोक से कुछ बाहर कोई चीज़ है तो यह तो अजीब-सी अवधारणा है, शहर के लोग पूछ सकते हैं कि वे लोक से बाहर क्यों हैं? आप लोक हैं और हम क्या हैं? यह तो नहीं हो सकता। लोक की प्रचलित अवधारणा से मैं सहमत नहीं हूँ।
आपको लगता है कि समकालीन हिंदी कविता नागरबोध की कविता है? यदि ऐसा है, तब समकालीन कविता इसकी परंपरा कहाँ से ग्रहण करती है?
मुझे याद पड़ता है कि मैंने ‘कविता का शहर’ में यह लिखा है कि कविता विधा के रूप में एक नागर विधा है, बुनियादी रूप से। संस्कृत की कविता में नगर केंद्र में है या आरण्यक समाज। वाल्मीकि की कविता का केंद्र क्या है? अयोध्या। अयोध्या नगर है। राजधानी है। राम की, दशरथ की राजधानी है, सारी राम कथाएँ नगर केंद्रित हैं। या उनका एक बड़ा हिस्सा आरण्यक समाज के बीच घटित होता है। जब राम को वनवास दिया जाता है, राम को गाँव नहीं भेजा जाता, वन-वास में जाते हैं राम। तो राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा आरण्यक समाजों के बीच कटता है या उनका बचपन और रावण-वध के बाद राम अयोध्या ही वापस आते हैं। रामराज्य अयोध्या में ही स्थापित होता है। रामकथा वस्तुतः कृषि सभ्यता के पैदा होने की कथा है। सीता उसी का प्रतीक है। राम उसी के प्रतीक हैं। राक्षस जिसे कहा गया वह तो रक्ष्य संस्कृति के लोग थे, जो जंगल काटे जाने के विरुद्ध थे। तो यह नई कृषि सभ्यता के विकास और जंगलों की रक्षा करते समाज के बीच टकराव की भी कथा है। लोकगीत को ग्रामीण कविता कह सकते हैं। बाक़ी जो अधिकांश कविता है या जो संस्कृत की कविताएँ हैं, वे भी नगरीय कविताएँ ही हैं। कविता की परंपरा वस्तुतः नगरीय कविता की ही परंपरा है।
कविता का शहर और शहर एक भिन्न अवधारणा है, कैसे?
रचना में आप जब यथार्थ का पुनर्सृजन करते हैं तो हर चीज़ का पुनर्सृजन होता है। समय भी पुनर्सृजित होता है। इसी तरह जब एक शहर उसमें आता है, तब वह पुनर्सृजित होता है। यह तय है कि यह वही शहर नहीं है जो बाहर है, यह एक अलग शहर है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर अभी तक जो शहर दिखाई देता है, तय है कि वह उतने आदर्श शहर नहीं रहे होंगे जितने हमारी क्लासिक रचनाओं में दिखाई देते हैं। तो वे ऐसे नगर हैं जो क्रिएट किए गए… वे पुनर्सृजित नगर हैं। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण या कालिदास की रचनाएँ हों, उनमें उनके कथानकों की ज़रूरत के अनुसार नगर पुनर्सृजित किए गए होंगे। कविता के अंदर आया शहर ठीक वही शहर नहीं होता जो बाहर है। एक तो क्या है कि यूं भी शहर इतना बड़ा होता है। बॉम्बे इतना बड़ा शहर है। उसके इतने सारे हिस्से हैं। उसे कई-कई हिस्सों में देखा जा सकता है। जैसे केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्ति है—“तुम इसे देखना कभी सुलगते क्षण में / यह अलग-अलग दिखता है हर दर्पण में” मतलब आप जितनी जगह से देखेंगे शहर को वह एक अलग शहर भी दिखेगा तो इसलिए कविता में वह पुनर्सृजित होता है। इसलिए वह वास्तविक शहर से भिन्न शहर होता है।
शहर पर बादशाह, समाज-विज्ञानी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार सोचते हैं। बादशाह और उसके अमले शहर को पाबंद बनाते हैं, उसके उपाय खोजते हैं। एक कवि के रूप में आप शहर को किस प्रकार देखते हैं?
शहर को हर आदमी अपने ढंग से देखता है। जैसे सत्ता अपने ढंग से देखती है। इसलिए आप अक्सर पाएँगे कि शहर के सबसे उन्नत और सबसे चमकीले हिस्से वे होते हैं, जो सत्ता के प्रतिदिन के उपयोग में आने वाले हिस्से होते हैं। जहाँ उनके घर होंगे, जहाँ उनके कार्यालय होंगे, जहाँ एरोड्रोम या रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले मार्ग होंगे जो उनके घर तक या कार्यालय तक पहुँचते हैं। तो वे मार्ग और वे सब जगहें बहुत ही अलग तरह की होंगी। जब एक व्यापारी देखेगा तो उन हिस्सों की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देगा जो व्यापारिक केंद्र हैं और तय है कि जब एक लेखक ढूँढ़ेगा तो वह अक्सर उन हिस्सों को देखेगा, जहाँ सबसे बड़ी संख्या में सबसे निचले वर्ग के लोग रहते हैं। जिनका जीवन आज भी बहुत विपन्नताओं में बीत रहा है। वह समाज के अंतर्विरोध को समझने के लिए शहर के सत्ताधारी वर्ग के रिहाइशी हिस्सों और श्रमशील निर्धन आबादी की बसावट वाले हिस्सों के फ़र्क़ को देखेगा। वह उन हिस्सों को भी देखेगा, जिनमें थोड़ा अवकाश होता है। जहाँ आराम से कुछ देर बतियाया जा सके, रहा जा सके, जहाँ वह बातचीत कर सके… लेखक ऐसे हिस्सों को ज़्यादा देखता है।
इसलिए ऐसा होता था कि बहुत सारे हिस्से होते थे हमारे शहर में जहाँ दिन भर लोग शतरंज खेल रहे हैं या रात में शतरंज खेल रहे हैं। चायघरों के कमरों में बैठे हुए हैं और उनमें कैरमबोर्ड रखे हुए हैं… तो इस तरह की जगह जहाँ एक अवकाश होता है, जहाँ एक तरह की स्पेस होती है—बतियाने-बातचीत करने की। इसलिए कॉफ़ी हाउसेज जो बने, कॉफ़ी हाउसेज की सारी अवधारणा जो है वह इसी तरीक़े की थी कि उसमें आ के बुद्धिजीवी बैठेंगे, अलग-अलग तबके के लोग बैठेंगे यह नहीं था कि कॉफ़ी पी ली तो आप जाइए। ऐसा नहीं था। आप कितनी भी देर बैठे रह सकते हैं। आप हो सकता है कि दिन भर बैठे रहें और दिन भर में आठ-दस कॉफ़ी पी लें। हम लोग कॉफ़ी हाउसेज में देखते थे कि कुछ लोग सुबह भी दिखते थे, शाम को भी दिखते थे। कॉफ़ी हाउस उस तरह की स्पेस बनाई गई जिसमें पढ़े-लिखे लोग जो बौद्धिकता के कामों से जुड़े थे, वे आकर वहाँ बैठ सकें और बहसें कर सकें। इस तरह के कॉफ़ी हाउसेज सारी दुनिया में बने। कहा जाता है कि सार्त्र की एक टेबल हुआ करती थी—फ़्रांस के कॉफ़ी हाउस में और वह उसी पर बैठते थे।
क़िस्सों का स्पेस ख़त्म होता जा रहा है। क्या कविता में भी क़िस्सों का स्पेस ख़त्म हो रहा है?
जीवन जैसा भी है—बदलेगा। जीवन में जिस तरह के भी बदलाव होंगे, वह रचना में भी प्रतिबिंबित होंगे। सीधे नहीं। ऐसा नहीं होता कि अभी आज जीवन बदला और अभी आज कविता में दिखने लगा या कहानी में दिखने लगा। लेकिन फिर भी जैसे नब्बे के बाद का जो दृश्य बदला उसमें जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए, टेक्नोलॉजी के आने से जो बड़े परिवर्तन हुए, सोवियत संघ के विघटन आदि सब मूल मुद्दे हैं। जो परिवर्तन हुए उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो था जिसने काफ़ी तंग किया या जिसने बहुत सारी चीज़ों को बदला ख़ासतौर से लेखक के लिए समस्याजनक परिवर्तन था कि समय की गति बदल गई और यह जो समय की गति बदलना है इसने बड़ी विकट स्थिति पैदा की, क्योंकि जो बीसवीं शती का समय था, नब्बे से पहले का वह सब कुछ के बावजूद उसमें एक तरह का थोड़ा धीमापन था। एकदम कंप्यूटर के आने से बिल गेट्स का जो विंडो आ गया, पहले तो कंप्यूटर सुनते थे तो लगता था कोई बड़ा हव्वा-सी चीज़ है; पर बिल गेट्स के विंडोज आने से उसे मध्यवर्ग के हर घर की चीज़ बना दिया गया। तो इससे एकदम चीज़ें बदल गईं। जिन जगहों पर लाइनों में लगना पड़ता था, वहाँ आपको मिनट दो मिनट लगने लगे… तो यह जो परिवर्तन है, इसमें एक बड़ा फ़र्क़ आया; रचना में भी उसके रिफ़्लेक्शन दिख रहे हैं, पर अभी थोड़ा समय और लगेगा।
इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल गतिकी से संबंधित है कि शहर की गतिकी को कविता कैसे पकड़ती है? यह प्रश्न अब सिर्फ़ शहर की गतिकी के बारे में ही नहीं, अपितु हमारे समय की गतिकी के बारे में भी है कि कविता इसको कैसे पकड़ती है?
गति कई कई रूप में अपने को रिफ़्लेक्ट करती है, जैसे अभी यह नया फ़ोन जब आया 2000 के बाद, स्मार्टफ़ोन जिसे हम कहते हैं—2010 के बाद लगभग, उससे आपके हाथ में एक ऐसा एपरेटस आ गया जिसमें सारी सूचनाएँ मौजूद हैं। एक बटन पर सारी सूचनाएँ प्रस्तुत हैं। हम लोगों को बचपन में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती थीं। तारीख़ें रटनी पड़ती थीं—इतिहास की। अब वह जो मेमोरी बॉक्स था, आपके दिमाग़ का, उसका वह हिस्सा अब ख़ाली हो गया; क्योंकि आपको अब रटना नहीं है। आपको अब यह मालूम करना है कि अकबर का पीरियड क्या है तो एक बटन दबाइए तो मालूम पड़ जाएगा कि अकबर का समय क्या है—यानी जितनी सूचनाएँ और संबंधित तथ्य हैं, वे अब आपकी उँगलियों की पोरों पर उपलब्ध हैं।
मेमोरी बॉक्स का जो सूचनाओं से भरा रहने वाला हिस्सा था, जिसे आप रट-रटकर भरते थे; वह एक तरह से एकदम ख़ाली हो गया। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि सूचना और स्मृति का जो रिश्ता था, वह बदला है। जब सूचना और स्मृति का रिश्ता बदलेगा तो स्मृति और सृजन का रिश्ता भी उससे कहीं न कहीं प्रभावित होगा। रचना तो मूलतः सृजन और स्मृति से संबंधित है, जो किसी भी रचना का बहुत ही महत्त्वपूर्ण पक्ष है। तो यह भी यानी यह हाइपोथेटिकल लग सकता है… इस तरह देखने के लिए बहुत सारी खोज-ख़बर से गुजरना पड़ेगा, विश्लेषण करना होगा। स्मृति और सृजन का संबंध बदल रहा है और इसी से मालूम पड़ेगा कि जो गति है सारी चीज़ों की वह कैसे बदल रही है।
यानी इसको इस तरीक़े से भी कहा जा सकता है कि क्या गतिकी स्मृति-भ्रंश का एक सबसे बड़ा कारण है?
स्मृति-भ्रंश कहना ग़लत होगा। ज्ञान का नहीं, सूचना का हिस्सा ख़ाली हो रहा है। ज्ञान और सूचना का जो भेद है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। व्याख्या ज्ञान से संचालित होती है। अब जैसे कहा जा रहा है कि 2026 तक कंप्यूटर कविताएँ वग़ैरा सब लिखने लगेगा। हालाँकि यह बात बहुत हाइपोथेटिकल है। यह सब बहुत काल्पनिक है, क्योंकि सृजन एक ऐसी चीज़ है जो बिना मनुष्य के नहीं संभव है, मतलब वह मैकेनिकल सृजन हो सकता है; पर मैकेनिकल सृजन का कोई अर्थ बहुत दूर तक तो नहीं हो सकता।
आपके कथेतर गद्य को देखें, उसका जो अधिकतर हिस्सा है वह स्मृतियों से निर्मित हुआ है। उसमें लोगों की स्मृतियाँ हैं, उसमें शहरों की स्मृतियाँ हैं, क्या कविता में इन स्मृतियों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था कि आपको गद्य में आना पड़ा? क्या कविता उन स्मृतियों के लिए मुफ़ीद जगह नहीं थी?
नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित ही कविता में… कविता तो बिना स्मृति के नहीं होती। कविता का वह एक बड़ा हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है। पूरी दुनिया में कवियों ने गद्य लिखा। गद्यकारों ने कविता नहीं लिखी। ज़्यादातर मतलब लिखने को तो बहुत सारे गद्यकार यहाँ पर भी लिख रहे हैं, पर सामान्यतः गद्यकार को यह आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह कविता में जाए। जबकि मूल विधा तो कविता ही है। कविता से ही सारी विधाएँ निकलीं—चाहे आख्यान हो, चाहे नाटक हो, आलोचना हो।
कविता तो मूल विधा है, पर कविता एक ऐसी विधा भी है; यानी वह भाषा का एक ऐसा अनुशासन है कि उसमें जीवन का बहुत सारा अनुभव ऐसा होता है कि उसे कविता में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप पाएँगे कि दुनिया के तमाम कवियों ने अच्छा गद्य लिखा और बहुत बड़ी मात्रा में गद्य लिखा। तो यह आवश्यक होता है कि एक कवि सारा बोझ अपनी कविता पर न डाले, बल्कि वह कुछ और रास्ते खोल सके। हालाँकि कोई भी कवि जब गद्य लिखता है तो वह भी कविता का ही विस्तार होता है। सामान्यतः वह वैसा गद्य नहीं होता जैसा एक गद्यकार का गद्य होता है। इसलिए आप कवियों का गद्य अलग से पहचान सकते हैं कि यह कवि का गद्य है। यह ऐसा विस्तार है जिसमें उसके बहुत सारे अनुभव या बहुत सारी जानकारियाँ चली जाती हैं।
‘चाँद की वर्तनी’ में कुछ प्रेम-कविताएँ हैं, लेकिन हिंदी का जो लोकवृत्त है; वह ज़्यादातर आपको आपकी राजनैतिक कविताओं के मार्फ़त याद रखता है। हिंदी लोकवृत्त और आलोचना ने इस तरफ़ कम ध्यान दिया है। आपकी कविताओं का मूल स्वर क्या है?
हमारे यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है और हमारे यहाँ क्या, शायद बहुत सारी जगहों पर और इस पर अलग से मैंने नोट्स लिए हैं। एक जो चर्चित कविता हो जाती है उसकी आड़ में बहुत कुछ ओट हो जाता है, अलक्षित रह जाता है। जैसे सुभद्राकुमारी चौहान की ‘झाँसी की रानी’ एक चर्चित कविता है। सुभद्रा जी ने और भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने बहुत सुंदर कहानियाँ लिखीं। उन्होंने बहुत सुंदर दूसरी तरह की कविताएँ लिखीं, पर वह सब कहीं न कहीं अलक्षित रह जाती हैं और जब भी कभी सुभद्रा जी की बात होती है तो ‘ख़ूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी’ से बाहर नहीं होती।
इससे दो तरह के नुक़सान हुए। एक तो कवि का बहुत सारा अच्छा हिस्सा ओट हो जाता है। दूसरा यह भी कि आप उस कविता की कभी भी बहुत बेहतर व्याख्या नहीं करते। उस पर अलग-अलग दृष्टियों से विचार नहीं करते। उसका विश्लेषण नहीं करते। अगर किसी से पूछा जाए कि हिंदी में गाथा-कविता, जो अच्छी गाथाएँ लोगों को याद हों; ऐसी कितनी गाथा-कविताएँ लोगों को याद हैं। अक्सर ऐसी दो कविताएँ एकाएक याद आती हैं, एक : ‘हल्दी-घाटी’ श्यामनारायण पांडे की और दूसरी सुभद्रा जी की ‘झाँसी की रानी’… और इन दोनों का कहीं कोई बहुत अच्छा विश्लेषण नहीं मिलता, जिसमें इनके शिल्प और संरचना पर विचार किया गया हो। यह एक कवि के साथ बड़ी समस्या है कि एक जो चर्चित कविता है, उसकी ओट में दूसरा छिप जाता है।
तमाम सर्जकों ने आलोचना लिखी है। आलोचना करते हुए कमोबेश उन्होंने अपने लिए जो काव्य-प्रतिमान चुने हैं, उन्हीं प्रतिमानों को आलोचना का प्रतिमान बनाया ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या कारण है कि एक रचनाकार को आलोचना के क्षेत्र में आना पड़ता है और यह कितना उचित है कि वह अपने रचनात्मक प्रतिमानों को केंद्र में रखकर आलोचना के प्रतिमानों का विकास करे?
आप पाएँगे कि जो रचनाकार आलोचक हैं और जो आलोचक हैं इसका एक जो बड़ा भेद मुझे लगता है कि रचनाकार जब आलोचक होता है तो वह थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, आत्मनिष्ठ होता है। आलोचक जब आलोचना करता है, तब वह थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए यह दोनों आलोचना के स्वभाव से भिन्न होते हैं।
रचनाकार जब आलोचना कर रहा है तो कहीं न कहीं अवचेतन रूप से या चेतन रूप से वह अपनी कविता या जो उसने रचा है उसको प्रमाण बनाने या उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है, चाहे वह अपनी कविता का उदाहरण न दे, लेकिन कहीं न कहीं उसके अवचेतन में अपनी किसी न किसी कविता की गूँज बनी रहती होगी। लेकिन यह सिर्फ़ एक पक्ष है इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत-सी जगहों पर कविता-आलोचक ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे कि ख़ुद रचनाकार भी दूसरे रचनाकार से सीख रहा होता है। वहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि वह अपने ही प्रतिमानों को हमेशा प्रतिमान बनाए क्योंकि हर रचनाकार बहुत सारे लोगों को पढ़ता है।
जैसे आप निराला को पढ़ रहे हैं, त्रिलोचन को पढ़ रहे हैं, नागार्जुन को पढ़ रहे हैं, शमशेर को पढ़ रहे हैं या और बहुत सारे लोगों को पढ़ रहे हैं तो तय है कि आप उनसे सीख भी रहे हैं। उनकी रचना के जो मूल्य हैं, वे कहीं न कहीं आप आत्मसात कर रहे होते हैं, तो दोनों तरह की स्थितियाँ दिखाई देंगी। हमेशा यह नहीं होता कि कवि सिर्फ़ अपने को ही जस्टिफ़ाई करे। अपनी रचनाओं के ही प्रतिमानों को सब पर लागू करे। इसलिए रचनाकार की आलोचना आलोचक से थोड़ी-सी भिन्न होती है। थोड़ी-सी क्या, बल्कि इस मामले में काफ़ी भिन्न होती है कि वह कहीं न कहीं थोड़ा सब्जेक्टिव होती है—आलोचक की तुलना में।
आज की कविताओं में मौजूद राजनैतिक प्रतीकों में एक समानता है और एक प्रकार अस्पष्टता भी। आप इसे कैसे देखते हैं?
ऐसा बहुत बार होता है, जैसे यह समय ज़्यादा राजनीतिक उथल-पुथल का समय है। लोकतंत्र का जो ढाँचा तैयार हुआ था इस समय उस पर राजनीतिक संकट दिख रहा है। इस समय जो राजनीतिक प्रतिरोध की रचना लिखी जाएगी, उसका एक बड़ा हिस्सा वह होगा जो चल रहे मुहावरों और जुमलों का इस्तेमाल करेगा, शिल्पगत भी उसमें एकजैसापन दिखेगा। यह हमेशा होगा। इसे आप अस्मिता-विमर्शों में भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। जितने अस्मिता-विमर्श हैं, उनकी भी यह समस्या है। उनके अंतर्गत लिखी जा रही रचनाओं में बहुत एक जैसा ट्रीटमेंट है। क्लीशे बन जाते हैं। लेकिन उसी में से आप जो अधिक अच्छा, प्रतिभाशाली है या कुछ अलग कर सकता है; वह उसी में से निकल आता है। अपनी अलग पहचान बनाता है।
क्या भक्तिकाल में सिर्फ़ चार-पाँच कवि थे—कबीर, मीरा, तुलसी, सूरदास, जायसी? एकाध हज़ार कवि तो रहे ही होंगे। ज़्यादा ही रहे होंगे। तो उसमें से छँटकर ये कवि आए, वहाँ भी यह एकजैसापन की समस्या रही होगी। छायावाद में भी सिर्फ़ चार कवि तो नहीं रहे थे। अनेक कवि रहे होंगे। तो हर दौर में अनेक कवि होते हैं। तीन सप्तक निकले। तीन सप्तक में इक्कीस कवि हैं और इनमें में से जब ढूँढ़ने जाते हैं तो पाँच या छह कवि से ज़्यादा याद नहीं आते। तो ऐसे बहुत सारे कवि एक समय में आते हैं। एक समय की कुछ कॉमन प्रवृत्तियाँ होती हैं, कुछ कॉमन प्रतीक होते हैं, एक क़िस्म की भाषा बन जाती है। उसमें से वही रचनाकार महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जो अपनी रचना के लिए अलग राहों का अन्वेषण कर लेता है।
इसलिए प्रतिरोध की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूरे विश्व की कविता में मिलती-जुलती-सी लगती हैं। बीसवीं सदी में एक समय आया, जिसमें सबसे क्रूर तानाशाह हुए। तानाशाह पर कुछ अच्छे कवि जैसे अर्नेस्तो कार्देनाल की एक कविता है—‘सोमोज’। तो तानाशाहों का कहीं-कहीं सीधे नाम लेकर कविता में उपयोग किया गया। हिटलर के नाम का प्रयोग किया गया। कहीं वह अमूर्त हो गया। अमूर्तता का रास्ता कॉमन प्रवृत्तियों की ओर चला जाता है।
आज के नए कवियों को आप कैसे देखते हैं?
लिखना बहुत ही कठिन काम है। इस समय लिखने वाले रचनाकारों की संख्या कुछ अधिक है। हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया, यानी सत्तर के दशक में तब पत्रिकाएँ बड़ा काम कर रही थीं। उनमें बहसें चल रही थीं और उनमें कविता के विशेषांक निकल रहे थे। कहानी के अंक निकल रहे थे। तो संभावनाशील रचनाकार कुछ ही समय में पहचान लिए जाते थे। छँटाई हो जाती थी। ‘पहल’ ने दो कविता-अंक निकाले। बहुत सारी अन्य पत्रिकाओं के भी कविता-अंक निकले।
इस समय यह काम पत्रिकाएँ नहीं कर रहीं। यह काम संगठन नहीं कर रहे कि नए संभावनाशील रचनाकार रेखांकित हो सकें। हिंदी का यह समय कई मायनों में विशिष्ट है। इसमें रचनाकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आदि काल से लेकर अस्सी तक का समय जिसमें कविता में स्त्रियाँ उँगलियों में गिनी जाने लायक़ हैं। पूरे भक्तिकाल में आप ले-देकर मीरा को याद करते हैं और छायावाद में महादेवी वर्मा या सुभद्राकुमारी चौहान को याद करते हैं। इक्कीस कवि हैं तीनों सप्तक में, एक कवयित्री हैं—शकुंत माथुर। गद्य में यह स्थिति नहीं थी। गद्य में स्त्रियाँ थीं और बहुत शक्तिशाली यानी कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे और बहुत सारे नाम थे, पर कविता में ऐसे नाम नहीं थे। सुभद्रा जी के बाद आपको ढूँढ़ने पड़ते थे नाम। तो यह जो वर्तमान है यानी अस्सी के बाद का जो समय है, ख़ासतौर से नब्बे के बाद कहना चाहिए, उसमें तो कवयित्रियाँ बहुत हैं और इन्हें रेखांकित करने का काम कौन कर रहा है? कौन सचमुच नई ज़मीन तोड़ रहा है? किसके यहाँ नए बिंब आ रहे हैं? इसको देखने-जाँचने-परखने का काम लगभग नहीं है।
समकालीन हिंदी कविता का प्रस्थान बिंदु आप कहाँ से मानते हैं?
कविता के लिए समकालीन जैसे विशेषण की शुरुआत सत्तर के दशक से होती है।
कैसे?
सत्तर के आसपास राजनीतिक परिदृश्य में कई बड़े परिवर्तन हुए। 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस का विभाजन ही नहीं होता, पहली बार पूँजीपति घराने कांग्रेस से अलग हुए हिस्से अर्थात् कांग्रेस (ओ) के साथ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस (ओ) जिसमें मोरारजी देसाई, निजलिंगगप्पा आदि वरिष्ठ कांग्रेसी थे, ही अल्टीमेटली सत्ता प्राप्त करेगी। उनका अनुमान लेकिन ग़लत हो गया। शायद सत्तर या इकहत्तर में जो चुनाव हुआ, उसमें इंदिरा गांधी को बहुमत मिला। इंदिरा गांधी नेहरूवियन इकॉनोमी को बदलती हैं और पहली बार नव-धनाढ्य वर्ग यानी नई लाइसेंस पॉलिसी से पैदा हुआ नया धनाढ्य वर्ग दृश्य पर आता है। नव-धनाढ्य यानी जब पावर में आता है तो उसमें और बड़े पूँजीपति घरानों के बीच टकराव पैदा होता है।
इसलिए ‘सारिका’ में एक धारावाहिक रूप से कमलेश्वर नव-धनाढ्यों की संस्कृति पर संपादकीय लिखते हैं। कमलेश्वर नव-धनाढ्यों को लगभग सांस्कृतिक रूप से विपन्न क़रार देते हुए उनका मज़ाक उड़ाते हैं। आप पाएँगे कि जो नव-धनाढ्य आ रहे थे, उनकी कोई कल्चरल रूट्स नहीं थीं। पुराने धनाढ्यों के पास क्लासिकल कलाओं की परंपरा थी। नव-धनाढ्य ने सुगम संगीत और ग़ज़ल को इस्टैब्लिश करने का काम किया। कह सकते हैं कि एक क़िस्म के लोकप्रिय कला-रूपों को अपना आधार बनाया। सत्तर के दशक में अचानक ग़ज़ल लिखे जाने का चलन बढ़ा। हर भाषा में ग़ज़ल लिखी जाने लगी। ग़ज़ल गायक बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे। सत्तर एक ऐसी समय-सीमा है, जहाँ पुराने नेहरू युग का जो असर चला आ रहा था, उसमें कहीं न कहीं ब्रेक लगता है। यह साठोत्तरी के नेहरू युग से मोहभंग से अलग है।
इंदिरा गांधी ने इसे परोक्ष रूप से स्वीकार किया। उनसे जब पूछा गया कि आप में और नेहरू में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा नेहरू एक राजनीतिक-चिंतक थे और मैं पॉलिटिशियन हूँ। उन्होंने नेहरू एरा की राजनीति के सारे पर्दे हटा दिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहीं न कहीं हुआ और यह ऐसा परिवर्तन था जो भारतीय समाज में एकदम नई हलचल पैदा कर रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी के लिए उस समय यह आवश्यक था—जनता का विश्वास जीतने के लिए—कि वह बहुत सारे लेफ़्ट मुहावरे बोलतीं और वही उन्होंने किया। उन्होंने वाम के तेवर अपनाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवीपर्स बंद करना यह सारे काम उन्होंने किए। लेकिन इंदिरा गांधी के विरुद्ध राजनीतिक शक्तियाँ भी शक्तिशाली हो रही थीं।
जयप्रकाश आंदोलन और हाइकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव पर दिए गए निर्णय ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। आपातकाल लागू हो गया और यह भारतीय जनतंत्र के इतिहास की पहली घटना थी, जिसमें अभी तक की सारी जनतांत्रिक स्वतंत्रताएँ एक झटके से ख़त्म कर दी गईं। सत्तर का जो दशक था पचहत्तर तक आते-आते यानी मध्य तक आते-आते एक तरह से हमारे जनतंत्र में पहली बार यह ख़तरा सामने आया कि जब भी पूँजी पर कोई संकट रहेगा तो वह कभी भी तानाशाही की तरफ़ जा सकता है। यह एक बड़ा परिवर्तन है। इमरजेंसी से थोड़ा पहले से समकालीन कविता की शुरुआत होती है, पर इमरजेंसी के बाद का जो पूरा समय है, उसे डिमार्केशन लाइन या प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए जहाँ से कविता के लिए समकालीनता जैसे शब्द की शुरुआत होती है।
समकालीन कविता के आरंभ में पूर्ववर्ती कविताओं से अलग किन लक्षणों को देखा जा सकता है?
कई नई प्रवृत्तियों को लक्ष्य किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने लेख भी लिखे। एक बड़ा परिवर्तन था कि एक जो नायक होता था, धूमिल की कविता तक आएँ तो धूमिल की ‘पटकथा’ में जो भारत है वह फटे वस्त्र पहने हुए है, पर वह है नायक। ‘मोचीराम’ भी बहुत ऊँचाई से बोलता है। तो सत्तर के दशक की कविता ने इस नायक को कविता से विदा कर दिया और नायकों की जगह कविता में चरित्रों का आना शुरू हुआ। यह जनतंत्र का एक बड़ा लक्षण था। यहाँ से कविता अपने व्यवहार में भी जनतांत्रिक होना शुरू होती है।
यह बात प्रगतिवाद की कविता में भी थोड़ी-थोड़ी दिखाई देती है, पर पूरी तरह से नहीं। सत्तर के दशक की कविता एकदम बोलचाल की जो भाषा थी, उसको सीधा स्वीकार करती है। यह दूसरा बड़ा परिवर्तन होता है जो भाषा के स्तर पर होता है। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है, हिंदी की पूरी आलोचना नामवर जी का तो लेख ही है ‘व्यापकता और गहराई’, आलोचना के ज़्यादातर पद वर्टिकल एक्सिस के ही पद हैं।
सत्तर के दशक में वर्टिकल एक्सिस के जो पद थे उनका लोप हुआ और हॉरिजॉन्टल एक्सेस या क्षैतिज धरातल के पद आए। सत्तर के बाद की कविता वर्टिकल एक्सिस की नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की कविता है। वह आस-पास के जीवन को देखती है। यह वास्तविक रूप से जनतांत्रिक प्रक्रिया की कविता है। इस कविता की एक बड़ी ख़ूबी इसकी स्थानीयता है। आप किसी भी कवि को पढ़ते हुए जान सकते हैं कि उसकी ज़मीन क्या है।
जो कविता सत्तर के बाद शुरू होती है जिसे समकालीन कविता कहा जाता है, इसका अंत कहाँ है? क्या आज की कविता भी समकालीन कविता है और उसी तरह की प्रवृत्तियों का विस्तार है?
अस्सी-पच्चासी के आस-पास एक नई पीढ़ी आती है जिसमें बद्री नारायण, देवी प्रसाद मिश्र, कुमार अम्बुज, कात्यायनी, अनामिका, नीलेश रघुवंशी, श्रीप्रकाश शुक्ल, जितेंद्र श्रीवास्तव इत्यादि अनेक कवि हैं। नब्बे के बाद एक बड़ा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन हालाँकि कविता में पूरी तरह दर्ज नहीं होता, दिखता नहीं है; लेकिन वह हो रहा था—राजनीतिक धरातल, सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर। प्रौद्योगिकी में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। लॉन्ग नाइंटीज पर विस्तार से बहस की गई, लेकिन इस परिवर्तन के प्रमाण कविता में दिखाई नहीं दिए। लेकिन बाद की कविता में एक नया परिवर्तन आता है।
अदनान कफ़ील दरवेश की एक कविता है—‘सन् 1992’—उसकी पंक्तियाँ हैं : ‘‘जब मैं पैदा हुआ / अयोध्या में ढहाई जा चुकी थी एक क़दीम मुग़लिया मस्जिद / जिसका नाम बाबरी मस्जिद था…’’ तो यह प्रस्थान-बिंदु है यानी उसमें जो आदमी कह रहा है कि मैं जब पैदा हुआ तो यह हो चुका था। तो यह प्रस्थान बिंदु को बहुत स्पष्ट कर देता है। यह वह प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से चीज़ें बदल रही थीं और कविता भी बदल रही थी।
यानी समकालीन हिंदी कविता को हम 1970 से लेकर के 2014 तक की कविता कह सकते हैं?
नहीं, सत्तर-बहत्तर से नाइंटीज तक। जो परिवर्तन हो रहा है, अभी भले ही वह न दिखे; थोड़ी देर से दिखे, पर उसे रेखांकित करना चाहिए। 2014 तो कोई तारीख़ ही नहीं है।
क्या आज की कविता एक नई सदी की नई कविता है और यह समकालीन हिंदी कविता का ही विस्तार है?
किसी भी समय की कविता हो, उस कविता में आने वाले परिवर्तन या उस नई कविता का चेहरा केवल उस समय आई नई पीढ़ी के कवि ही नहीं बनाते हैं। उससे पहले के जो कवि हैं, जो लिख रहे होते हैं, वह भी कहीं न कहीं उसको बनाते हैं। यह नहीं है कि जो सत्तर के दशक से या उससे भी पहले से जो रचनाकार लिखते हुए आ रहे थे, उनका इस नई सदी की कविता का चेहरा-मोहरा बनाने में कोई योगदान नहीं है।
ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बात होगी तो आप न केदारनाथ सिंह को भूल सकते हैं और न कुँवर नारायण को।
भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कविता का चेहरा सिर्फ़ वह पीढ़ी नहीं बनाती जो उसी समय-अवधि में आई होती है। वह पीढ़ी और उसकी रचनात्मकता महत्त्वपूर्ण होती है। वह कुछ नया-टटका करती है। लेकिन वही सब कुछ नहीं करती। आप सोचिए कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ इतने सारे मार्क्सिस्ट थे इस देश में और यह सदी की बहुत बड़ी घटना थी, उस समय जो सबसे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिया, वह कुँवर नारायण ने दिया।
कुँवर नारायण से पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या समाजवाद का अंत हो गया है? वग़ैरा-वग़ैरा? तो कुँवर नारायण ने कहा कि “सत्ताओं के बदलने से विचारधाराएँ नहीं बदलतीं। सत्ता के अंत होने से विचारधाराओं का अंत नहीं होता।” यह बात कुँवर नारायण जैसा आदमी कह रहा था, जो मार्क्सिस्ट नहीं थे। तो इसी तरह किसी भी समय में उस समय की रचना का, उस समय की समझदारी का चेहरा और उसके नाक-नक़्श बनाने का काम, उस समय में काम कर रही कई पीढ़ियों के लोग करते हैं।
नए ब्लॉग
लोकप्रिय ब्लॉग
सबसे ज़्यादा पंसद किए गए ब्लॉग


