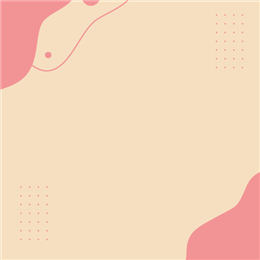असाध्य वीणा
asadhy wina
आ गए प्रियंवद! केशकंबली! गुफा-गेह!
राजा ने आसन दिया। कहा :
‘कृतकृत्य हुआ मैं तात! पधारे आप।
भरोसा है अब मुझको
साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी!’
लघु संकेत समझ राजा का
गण दौड़। लाए असाध्य वीणा,
साधक के आगे रख उसको, हट गए।
सभी की उत्सुक आँखें
एक बार वीणा को लख, टिक गईं
प्रियंवद के चेहरे पर।
‘यह वीणा उत्तराखंड के गिरि-प्रांतर से
—घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी—
बहुत समय पहले आई थी।
पूरा तो इतिहास न जान सके हम :
किंतु सुना है
वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस
अति प्राचीन किरीटी-तरु से इसे गढ़ा था—
उसके कानों में हिम-शिखर रहस्य कहा करते थे अपने,
कंधों पर बादल सोते थे,
उस की करि-शुंडों-सी डालें
हिम-वर्षा से पूरे वन-यूथों का कर लेती थीं परित्राण,
कोटर में भालू बसते थे,
केहरि उसके वल्कल से कंधे खुजलाने आते थे।
और—सुना है—जड़ उसकी जा पहुँची थी पाताल-लोक,
उस की ग्रंध-प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकि
सोता था।
उसी किरीटी-तरु से वज्रकीर्ति ने
सारा जीवन इसे गढ़ा :
हठ-साधना यही थी उस साधक की—
वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन-लीला।’
राजा रुके साँस लंबी लेकर फिर बोले :
‘मेरे हार गए सब जाने-माने कलावंत,
सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्प चूर,
कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका।
अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई।
पर मेरा अब भी है विश्वास
कृच्छ्र-तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था।
वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी
इसे जब सच्चा-स्वरसिद्ध गोद में लेगा।
तात! प्रियंवद! लो, यह सम्मुख रही तुम्हारी
वज्रकीर्ति की वीणा,
यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह :
सब उदग्र, पर्युत्सुक,
जन-मात्र प्रतीक्षमाण!’
केशकंबली गुफा-गेह ने खोला कंबल।
धरती पर चुप-चाप बिछाया।
वीणा उस पर रख, पलक मूँद कर, प्राण खींच,
करके प्रणाम,
अस्पर्श छुअन से छुए तार।
धीरे बोला : ‘राजन्! पर मैं तो
कलावंत हूँ नहीं, शिष्य, साधक हूँ—
जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी।
वज्रकीर्ति!
प्राचीन किरीटी-तरु!
अभिमंत्रित वीणा!
ध्यान-मात्र इनका तो गद्-गद् विह्वल कर देने वाला है!’
चुप हो गया प्रियंवद।
सभा भी मौन हो रही।
वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया।
धीरे-धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया।
सभा चकित थी—अरे, प्रियंवद क्या सोता है?
केशकंबली अथवा होकर पराभूत
झुक गया वाद्य पर?
वीणा सचमुच क्या है असाध्य?
पर उस स्पंदित सन्नाटे में
मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा—
नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था।
सघन निविड में वह अपने को
सौंप रहा था उसी किरीटी-तरु को।
कौन प्रियंवद है कि दंभ कर
इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे?
कौन बजावे
यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही?
भूल गया था केशकंबली राजा-सभा को :
कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था
जिसमें साक्षी के आगे था
जीवित वही किरीटी-तरु
जिसकी जड़ वासुकि के फण पर थी आधारित,
जिसके कंधे पर बादल सोते थे
और कान में जिसके हिमगिरि कहते थे अपने रहस्य।
संबोधित कर उस तरु को, करता था
नीरव एकालाप प्रियंवद।
‘ओ विशाल तरु!
शत्-सहस्र पल्लवन-पतझरों ने जिसका नित रूप सँवारा,
कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी,
दिन भौंरे कर गए गुँजरित,
रातों में झिल्ली ने
अनकथ मंगल-गान सुनाए,
साँझ-सवेरे अनगिन
अनचीन्हे खग-कुल की मोद-भरी क्रीड़ा-काकलि
डाली-डाली को कँपा गई—
ओ दीर्घकाय!
ओ पूरे झारखंड के अग्रज,
तात, सखा, गुरु, आश्रय,
त्राता महच्छाय,
ओ व्याकुल मुखरित वन-ध्वनियों के
वृंदगान के मूर्त रूप,
मैं तुझे सुनूँ,
देखूँ, ध्याऊँ
अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुत, निर्वाक् :
कहाँ साहस पाऊँ
छू सकूँ तुझे!
तेरी काया को छेद, बाँध कर रची गई वीणा को
किस स्पर्धा से
हाथ करें आघात
छीनने को तारों से
एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में
स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए!
‘नहीं, नहीं! वीणा यह मेरी गोद रखी है, रहे,
किंतु मैं ही तो
तेरी गोद बैठा मोद-भरा बालक हूँ,
ओ तरु-तात! सँभाल मुझे,
मेरी हर किलक
पुलक में डूब जाए :
मैं सुनूँ,
गुनूँ, विस्मय से भर आँकूँ
तेरे अनुभव का एक-एक अंत:स्वर
तेरे दोलन की लोरी पर झूमूँ मैं तन्मय—
गा तू :
तेरी लय पर मेरी साँसें
भरें, पुरें, रीतें, विश्रांति पाएँ।
‘गा तू!
यह वीणा रक्खी है : तेरा अंग-अपंग!
किंतु अंगी, तू अक्षत, आत्म-भरित,
रस-विद्
तू गा :
मेरे अँधियारे अंतस् में आलोक जगा
स्मृति का
श्रुति का—
तू गा, तू गा, तू गा, तू गा!
‘हाँ, मुझे स्मरण है :
बदली—कौंध—पत्तियों पर वर्षा-बूँदों की पट-पट।
घनी रात में महुए का चुप-चाप टपकना।
चौंके खग-शावक की चिहुँक।
शिलाओं को दुलराते वन-झरने के
द्रुत लहरीले जल का कल-निदान।
कुहरे में छन कर आती
पर्वती गाँव के उत्सव-ढोलक की थाप।
गड़रियों की अनमनी बाँसुरी।
कठफोड़े का ठेका। फुलसुँघनी की आतुर फुरकन :
ओस-बूँद की ढरकन—इतनी कोमल, तरल
कि झरते-झरते मानो
हरसिंगार का फूल बन गई।
भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर-ध्वनि।
कूँजों का क्रेंकार। काँद लंबी टिट्टिभ की।
पंख-युक्त सायक-सी हंस-बलाका।
चीड़-वनों में गंध-अंध उन्मद पतंग की जहाँ-तहाँ टकराहट
जल-प्रताप का प्लुत एकस्वर।
झिल्ली-दादुर, कोकिल-चातक की झंकार पुकारों की यति में
संसृति की साँय-साँय।
‘हाँ, मुझे स्मरण है :
दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़
हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ।
घरघराहट चढ़ती बहिया की।
रेतीले कगार का गिरना छप्-छड़ाप।
झंझा की फुफकार, तप्त,
पेड़ों का अररा कर टूट-टूट कर गिरना।
ओले की कर्री चपत।
जमे पाले से तनी कटारी-सी सूखी घासों की टूटन।
ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे-धीरे रिसना।
हिम-तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुप-चाप।
घाटियों में भरती
गिरती चट्टानों की गूँज—
काँपती मंद्र गूँज—अनुगूँज—साँस खोई-सी, धीरे-धीरे नीरव।
‘मुझे स्मरण है :
हरी तलहटी में, छोटे पेड़ों की ओट ताल पर
बँधे समय वन-पशुओं की नानाविध आतुर-तृप्त पुकारें :
गर्जन, घुर्घुर, चीख़, भूक, हुक्का, चिचियाहट।
कमल-कुमुद-पत्रों पर चोर-पैर द्रुत धावित
जल-पंछी की चाप
थाप दादुर की चकित छलाँगों की।
पंथी के घोड़े की टाप अधीर।
अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की।
‘मुझे स्मरण है :
उझक क्षितिज से
किरण भोर की पहली
जब तकती है ओस-बूँद को
उस क्षण की सहसा चौंकी-सी सिहरन।
और दुपहरी में जब
घास-फूल अनदेखे खिल जाते हैं
मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुँजार—
उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव।
और साँझ को
जब तारों की तरल कँपकँपी
स्पर्शहीन झरती है—
मानो नभ में तरल नयन ठिठकी
नि:संख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद—
उस संधि-निमिष की पुलकन लीयमान।
‘मुझे स्मरण है :
और चित्र प्रत्येक
स्तब्ध, विजड़ित करता है मुझको।
सुनता हूँ मैं
पर हर स्वर-कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख—
वायु-सा नाद-भरा मैं उड़ जाता हूँ।...
मुझे स्मरण है—
पर मझको मैं भूल गया हूँ :
सुनता हूँ मैं—
पर मैं मुझसे परे, शब्द में लीयमान।
‘मैं नहीं, नहीं! मैं कहीं नहीं!
ओ रे तरु! ओ वन!
ओ स्वर-संभार!
नाद-मय संसृति!
ओ रस-प्लावन!
मुझे क्षमा कर—भूल अकिंचनता को मेरी—
मुझे ओट दे—ढँक ले—छा ले—
ओ शरण्य!
मेरे गूँगेपन को तेरे साए स्वर-सागर का ज्वार डुबा ले!
आ, मुझे भुला,
तू उतर वीन के तारों में
अपने से गा—
अपने को गा—
अपने खग-कुल को मुखरित कर
अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बाँध,
अपने छायातप, वृष्टि-पवन, पल्लव-कुसमन की लय पर
अपने जीवन-संचय को कर छंदयुक्त,
अपनी प्रज्ञा को वाणी दे!
तू गा, तू गा—
तू सन्निधि पा—तू खो
तू आ—तू हो—तू गा! तू गा!’
राजा जागे।
समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था—
काँपी थीं उँगलियाँ।
अलस अँगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा :
किलक उठे थे स्वर-शिशु।
नीरव पदा रखता जालिक मायावी
सधे करों से धीरे-धीरे-धीरे
डाल रहा था जाल हेम-तारों का।
सहसा वीणा झनझना उठी—
संगीतकार की आँखों में ठंडी पिघली ज्वाला-सी झलक गई—
रोमांच एक बिजली-सा सबके तन में दौड़ गया।
अवतरित हुआ संगीत
स्वयंभू
जिसमें सोता है अखंड
ब्रह्मा का मौन
अशेष प्रभामय।
डूब गए सब एक साथ।
सब अलग-अलग एकाकी पार तिरे।
राजा ने अलग सुना :
जय देवी यश:काय
वरमाल लिए
गाती थी मंगल-गीत,
दुंदभी दूर कहीं बजती थी,
राज-मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का
ईर्ष्या, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुता
सभी पुराने लुगड़े-से झर गए, निखर आया था जीवन-कांचन
धर्म-भाव से जिसे निछावर वह कर देगा।
रानी ने अलग सुना :
छँटती बदली में एक कौंध कह गई—
तुम्हारे ये मणि-माणक, कंठहार, पट-वस्त्र,
मेखला-किंकिणि—
सब अंधकार के कण हैं ये! आलोक एक है
प्यार अनन्य! उसी की
विद्युल्लता घेरती रहती है रस-भार मेघ को,
थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है
आश्वस्त, सहज विश्वास भरी।
रानी
उस एक प्यार को साधेगी।
सबने भी अलग-अलग संगीत सुना।
इसको
वह कृपा-वाक्य था प्रभुओ का।
उसको
आतंक-मुक्ति का आश्वासन!
इसको
वह भरी तिजोरी में सोने की खनक।
उसे
बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोंधी खुदबुद।
किसी एक को नई वधू की सहमी-सी पायल ध्वनि।
किसी दूसरे को शिशु की किलकारी।
एक किसी को जाल-फँसी मझली की तड़पन—
एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की।
एक तीसरे को मंडी की ठेलमठेल, गाहकों की आस्पर्धा भरी बोलियाँ,
चौथे को मंदिर की ताल-युक्त घंटा-ध्वनि!
और पाँचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें
और छटे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की
अविराम थपक।
बटिया पर चमरौधे की रूँधी चाप सातवें के लिए—
और आठवें को कुलिया की कटी मेंड़ से बहते जल की छुल-छुल।
इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुँघरू की।
उसे युद्ध का ढोल।
इसे संझा-गोधूलि की लघु टुन-टुन—
उसे प्रलय का डमरू-नाद।
इसको जीवन की पहली अँगड़ाई
पर उसको महाजृंभ विकराल काल!
सब डूबे, तिरे, झिपे, जागे—
हो रहे वंशवद, स्तब्ध :
इयत्ता सबकी अलग-अलग जागी,
संघीत हुई,
पा गई विलय।
वीणा फिर मूक हो गई।
साधु! साधु!
राजा सिंहासन से उतरे—
रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल,
जनता विह्वल कह उठी ‘धन्य!
हे स्वरजित्! धन्य! धन्य!’
संगीतकार
वीणा को धीरे से नीचे रख, ढँक—मानो
गोदी में सोए शिशु को पालने डाल कर मुग्धा माँ
हट जाए, दीठ से दुलराती—
उठ खड़ा हुआ।
बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन,
बोला :
‘श्रेय नहीं कुछ मेरा :
मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में—
वीणा के माध्यम से अपने को मैंने
सब कुछ को सौंप दिया था—
सुना आपने जो वह मेरा नहीं,
न वीणा का था :
वह तो सब कुछ की तथता थी
महाशून्य
वह महामौन
अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय
जो शब्दहीन
सब में गाता है।’
नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केशकंबली।
लेकर कंबल गेह-गुफा को चला गया।
उठ गई सभा। सब अपने-अपने काम लगे।
युग पलट गया।
प्रिय पाठक! यों मेरी वाणी भी
मौन हुई।
- पुस्तक : सन्नाटे का छंद (पृष्ठ 113)
- संपादक : अशोक वाजपेयी
- रचनाकार : अज्ञेय
- प्रकाशन : वाग्देवी प्रकाशन
- संस्करण : 1997
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.